ऐसा होता है कि कोई श्रमण या ब्राह्मण बड़ा तार्किक और वैचारिक होता है।
वह अपनी तर्कबुद्धि से ठोक-पीटकर, जाँच-पड़ताल कर (व्यर्थ) निष्कर्ष निकाल, वैचारिक उड़ान भरते हुए (मिथ्या बातें) कहने लगता है… जैसे ‘आत्मा होती है’… या ‘आत्मा नहीं होती’… या ‘कर्म नहीं होते’… या ‘पुनर्जन्म नहीं होता’… या ‘निर्वाण नहीं होता’…
—गोतम बुद्ध (ब्रह्मजाल सुत्त)

क्या धर्म तार्किक है?
इसलिए सुनते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
और इसे अपनी सुविधा और गति से धीरे-धीरे पढ़ें।)
किसी बात के स्वीकार्य होने के लिए आजकल उसका ‘तार्किक’ होना लगभग अनिवार्य मान लिया गया है। आम धारणा यह बन चुकी है कि जो बात तार्किक है, वही सही होगी—मानो वह पत्थर की लकीर हो। अक्सर देखा जाता है कि यदि आप तर्क देकर अपनी बात समझाते हैं, तो लोग भली हो या बुरी, कोई भी बात मान लेते हैं। दूसरी ओर, बिना तर्क के कही गई अच्छी-से-अच्छी बात भी अस्वीकृत हो जाती है।
तर्क आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आधुनिक दुनिया में तर्क एक अतिरंजित और अनिवार्य गुण बन चुका है।
नास्तिक लोग अक्सर धर्म को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ‘तार्किक’ नहीं लगता। वहीं कई आस्तिक यह मानते हैं कि बौद्ध धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह तार्किक है। वे गर्व से कहते हैं— “बौद्ध धर्म आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए।”
यहीं एक गंभीर समस्या जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति धर्म को ‘तर्क’ के आधार पर स्वीकार करता है, तो वह वास्तव में धर्म को नहीं, बल्कि अपने तर्क को प्राथमिकता दे रहा होता है। ऐसी स्थिति में धर्म श्रद्धा या अनुभव का विषय न रहकर केवल एक बौद्धिक व्यायाम बन जाता है। और जिस दिन उसी धर्म का कोई गहरा सिद्धांत उस तर्क में फिट नहीं बैठता, वह उसे उतनी ही आसानी से अस्वीकार भी कर देता है।
कोई बात बहुत तर्कसंगत और विचारशील होती है, पर वह व्यर्थ, खोखली और मिथ्या होती है।
जबकि कोई बात तर्कसंगत और विचारशील नहीं होती, पर वह वास्तविक, यथार्थ और सच्ची होती है।
…तब कोई सच्चाई की रक्षा करने वाला समझदार पुरुष किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि ‘केवल यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।’
— गोतम बुद्ध (चङ्कीसुत्त)
तर्क—एक दुधारी तलवार
तर्क किसी बात को समझने में सहायक हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह अंधा भी हो सकता है। तर्क अक्सर एकतरफा होता है। वह सीधी रेखा में चलता है, जबकि वास्तविकता बहुआयामी होती है। तर्क काला-सफेद देखता है, पर जीवन अक्सर धूसर होता है।
इतिहास पर नज़र डालें तो स्पष्ट दिखता है कि दुनिया की सबसे विध्वंसकारी घटनाओं के पीछे पागलपन नहीं, बल्कि अत्यंत सुसंगत और “मज़बूत” तर्क मौजूद थे।
नाज़ीवाद कोई अचानक उठी हिंसक सनक नहीं थी। उसके पीछे यह तर्क था कि मानवता की उन्नति के लिए “श्रेष्ठ नस्ल” का जीवित रहना और “कमज़ोर नस्ल” का समाप्त होना आवश्यक है। साम्यवाद का तर्क सामाजिक न्याय और समानता का था—कितना पवित्र सुनाई देता है!—लेकिन उसे अंतिम सीमा तक खींचने पर उसने रक्तरंजित तानाशाहियाँ पैदा कीं। पूंजीवाद का तर्क आर्थिक विकास का था, पर उसकी अति ने एकाधिकार, उपनिवेशवाद और संसाधनों के लिए युद्धों को जन्म दिया।
सामाजिक डार्विनिज़्म ने यह मान्यता दी कि कमजोरों का मिट जाना न केवल स्वाभाविक है, बल्कि आवश्यक भी। मध्यकाल में स्त्रियों को ‘डायन’ या ‘सती’ बनाकर जलाने के पीछे भी तत्कालीन समाज का अपना एक “ठोस धार्मिक तर्क” था, जिससे बहुसंख्यक लोग सहमत थे।
आज भी यही होता है। जब किसी धार्मिक तर्क को उसकी सीमा से आगे खींचा जाता है, तो वह चरमपंथ बन जाता है। एक आतंकवादी भी जब बम फोड़ता है, तो उसके भीतर एक बहुत स्पष्ट और सुव्यवस्थित “धार्मिक तर्क” चल रहा होता है।
इसलिए कहता हूँ, कालामों। न सुनी-सुनाई बात मानो, न परंपरागत बात मानो, न अटकलेबाजी मानो, न शास्त्र-ग्रंथों की बात मानो, न तर्कसंगत कारण मानो, न अनुमानित कारण मानो, न समतुल्य परिस्थिति में लागू होती बात मानो, न अपनी धारणा से मेल खाती बात मानो, न संभावित बात मानो, न श्रमण गुरु के सम्मानार्थ मानो।
बल्कि कालामों, जब तुम्हें स्वयं पता चले—‘यह स्वभाव अकुशल है। यह स्वभाव दोषपूर्ण है। यह स्वभाव ज्ञानियों द्वारा निंदित है। यह स्वभाव मानने से, उस पर चलने से अहित होता है, दुःख आता है’—तब तुम्हें वह स्वभाव त्याग देना चाहिए।
— गोतम बुद्ध (अंगुत्तरनिकाय ३:६६ : केसमुत्तिसुत्त)
बौद्ध इतिहास का एक काला अध्याय
बौद्ध धर्म का इतिहास स्वर्णिम है, लेकिन उसमें एक काला अध्याय भी है। यहाँ उद्देश्य किसी ऐतिहासिक व्यक्ति पर दोषारोपण करना नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति को समझना है जहाँ तर्क अनुभव से ऊपर बैठ जाता है।
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ विद्वान और भाषाविद भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को अत्यधिक तार्किक ढाँचे में बाँधने का प्रयास किया। विशेष रूप से पाँचवीं शती के महान टीकाकार आचार्य बुद्धघोष ने बुद्ध की देशनाओं को एक कसे हुए तर्कतंत्र में प्रस्तुत किया। जो बात उस तर्क में फिट नहीं बैठी, उसे या तो गौण कर दिया गया या उसकी ऐसी व्याख्या की गई कि वह तर्कसंगत दिखे। इससे धर्म अधिक व्यवस्थित और बौद्धिक तो हुआ, लेकिन उसका लचीलापन और प्रयोगशीलता कम होती गई।
परिणाम यह हुआ कि नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में बौद्ध भिक्षु शास्त्रार्थ में अजेय हो गए, लेकिन दुःख-मुक्ति के लक्ष्य से दूर होते चले गए। धर्म की लोकप्रियता बढ़ी, पर उसकी फलदायिता घटती गई।
बुद्ध का उद्देश्य कभी तार्किक विवाद जीतना नहीं था। उन्होंने कई सूत्रों में भिक्षुओं को वाद-विवाद से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ सत्य से अधिक अहंकार सक्रिय हो जाता है। हमें धर्म को इसलिए नहीं अपनाना चाहिए कि वह तार्किक है, बल्कि इसलिए कि वह दुःख का अंत करता है।
इसी संदर्भ में जैन उदाहरण भी उल्लेखनीय है। जैन आचार्यों ने अहिंसा के तर्क को अत्यंत गंभीरता से पकड़ा—पानी छानकर पीना, मुँह पर पट्टी बाँधना, स्नान न करना। तर्क पवित्र था, लेकिन विवेक की कमी के कारण वह अव्यवहारिक हो गया और व्यापक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सका।
तर्क का उचित स्थान
यहाँ यह समझना आवश्यक है कि बुद्ध तर्क के विरोधी नहीं थे। वे तर्क को नकारते नहीं, बल्कि उसकी सीमा तय करते हैं। बुद्ध के यहाँ तर्क लक्ष्य नहीं, बल्कि एक औज़ार है—जो मन को अंधविश्वास, जड़ परंपराओं और जमी हुई धारणाओं से बाहर निकालने में सहायक होता है।
लेकिन जहाँ तर्क स्वयं सत्य होने का दावा करने लगे, वहीं वह अवरोध बन जाता है। बुद्ध तर्क का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि साधक अनुभव की ओर बढ़े, न कि अनुभव के स्थान पर तर्क को बैठा दे। तर्क यहाँ दीपक है—रास्ता दिखाने के लिए। परंतु चलना स्वयं साधक को ही पड़ता है।
समस्या तर्क नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तर्क को विवेक और अनुभव से ऊपर बैठा दिया जाता है।
विवेक: तर्क से ऊपर
विवेक जानता है कि हर स्थिति और हर समस्या का समाधान एक ही सैद्धांतिक फॉर्मूले से नहीं हो सकता।
उदाहरण के तौर पर चिकित्सा विज्ञान को देखें। तर्क कह सकता है— “यह दवा बीमारी ठीक करती है, तो ज़्यादा मात्रा में लो, जल्दी ठीक हो जाओगे।” यह सीधा और आकर्षक तर्क है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वही दवा गलत मात्रा में ली जाए तो ज़हर बन सकती है। सही मात्रा, सही समय और सही अवधि का ज्ञान तर्क से नहीं, विवेक और अनुभव से आता है।
बुद्ध के जीवन में भी यही बात दिखती है। गृहत्याग के बाद उन्होंने भी तर्क का सहारा लिया—यदि सुख ही दुःख का कारण है, तो सभी सुखों का त्याग कर देना चाहिए। यह एक पक्का तर्क था। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने छह वर्षों तक घोर कष्ट सहे, शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन कोई मनुष्योत्तर अवस्था प्राप्त नहीं हुई।
तब उन्होंने विवेक का सहारा लिया। तर्क के उस अतिवादी निष्कर्ष को एक-ओर रखकर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, संतुलित आहार स्वीकार किया, और उसी से आगे बढ़ते-बढ़ते बुद्धत्व प्राप्त किया।
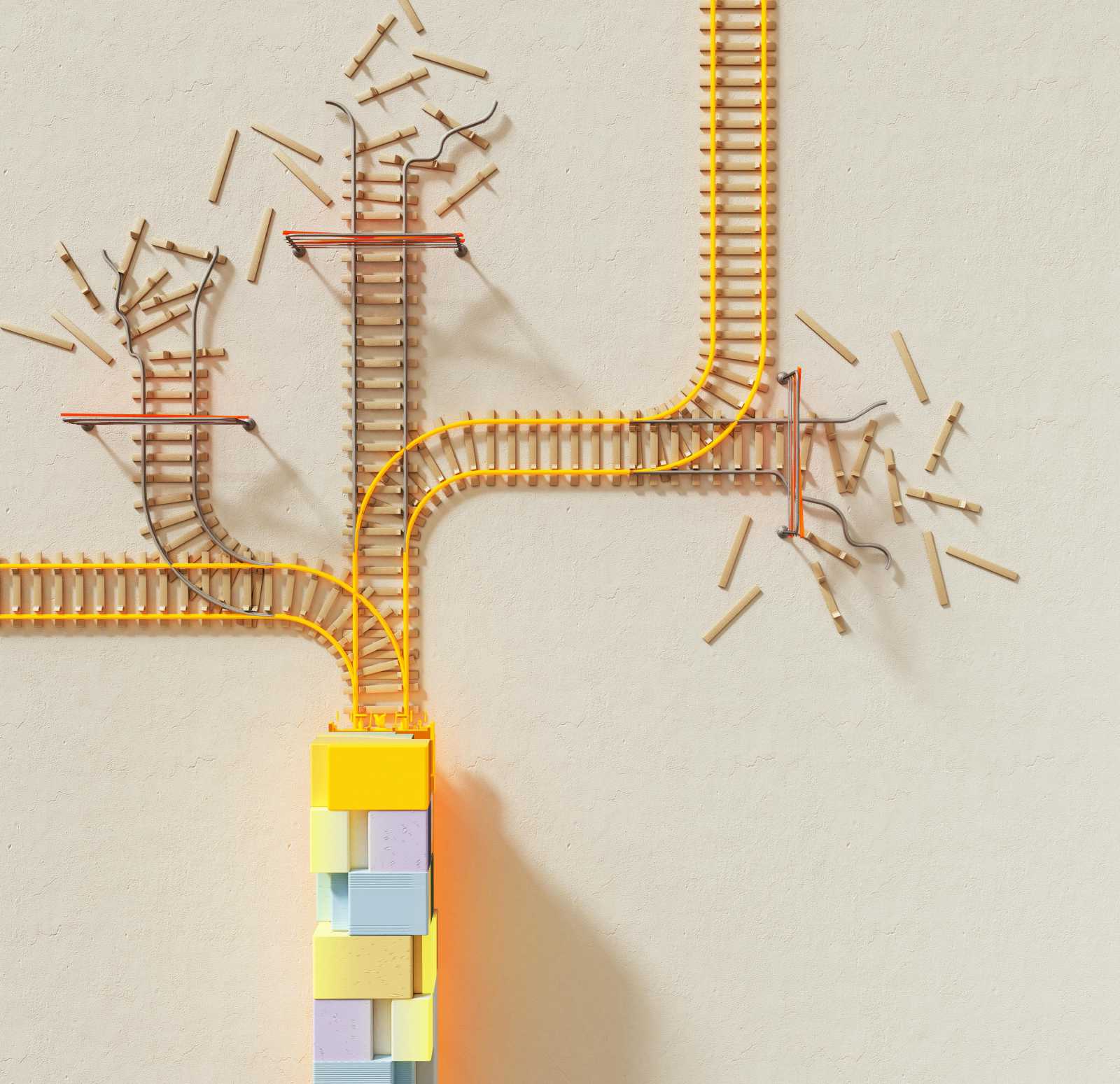
विवेक आता कैसे है
विवेक किसी एक क्षण में उत्पन्न नहीं हो जाता। यह कोई नैतिक आदेश नहीं है, बल्कि एक पकने वाली क्षमता है। शील से चित्त स्थूल विक्षेपों से मुक्त होता है, समाधि से स्थिर होता है, और प्रज्ञा से स्पष्ट होता है। इसी प्रज्ञा की परिपक्व अवस्था को विवेक कहा जा सकता है।
इसलिए बिना चित्त-शुद्धि के विवेक अक्सर केवल चतुराई बनकर रह जाता है—जो बाहर से सही दिखती है, पर भीतर से स्वार्थ और अहं से रंगी होती है।
विवेक सापेक्षतावाद नहीं है
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवेक का अर्थ यह नहीं कि “सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर है” या “जो मन में आए वही कर लो।” विवेक कर्म और परिणाम की स्पष्ट समझ से बंधा होता है। परिस्थिति बदल सकती है, उपाय बदल सकते हैं, लेकिन कसौटी नहीं बदलती—और वह कसौटी है: क्लेशों में वृद्धि या क्षय।
इस अर्थ में विवेक लचीला है, लेकिन दिशाहीन नहीं। विवेक कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। जब वह किसी व्यक्ति में उतरता है, तो वह कुछ ठोस गुणों के रूप में दिखाई देता है। बुद्ध ऐसे विवेकशील व्यक्ति को चार शब्दों में पहचानते हैं, जो केवल तार्किक व्यक्ति में नहीं मिलते:
- मत्तञ्ञु (मात्रा का ज्ञान): विवेकशील व्यक्ति जानता है कि किसी भी चीज़ की ‘सीमा’ क्या है। भोजन कितना करना है, बोलना कितना है, दवा कितनी लेनी है, सोचना कितना है, यहाँ तक कि साधना कितनी करनी है। हर रचित वस्तु की एक सीमा होती है।
- कालञ्ञु (समय का ज्ञान): वह जानता है कि किस बात को कहने या करने का ‘सही समय’ कौन सा है। सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए, तो वह अपना प्रभाव खो देती है। चाहे वह राजनीति हो या धर्म, ‘टाइमिंग’ ही सब कुछ है।
- अत्तञ्ञु (आत्म-ज्ञान): वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को भली-भांति जानता है। उसे पता होता है कि वह अभी कहाँ खड़ा है, इसलिए उसमें झूठा अहंकार नहीं होता। वह खुद को न तो ऊँचा मानता है और न ही नीचा।
- कतञ्ञु (कृतज्ञता): वह रूखा तार्किक नहीं होता, बल्कि उसे अपने लिए किए गए उपकारों का ज्ञान होता है। कृतज्ञता उसे विनम्र और स्मृतिमान बनाती है।
तर्क आपको एक सिद्धांत दे सकता है, लेकिन कब कौन सा सिद्धांत लागू करना है, यह केवल विवेक बता सकता है। कभी-कभी क्लेश हटाने के लिए कठोर मेहनत की ज़रूरत होती है, तो कभी सिर्फ़ एक शांत अवलोकन ही पर्याप्त होता है। यह भेद तर्क नहीं कर सकता, यह प्रज्ञा का काम है।
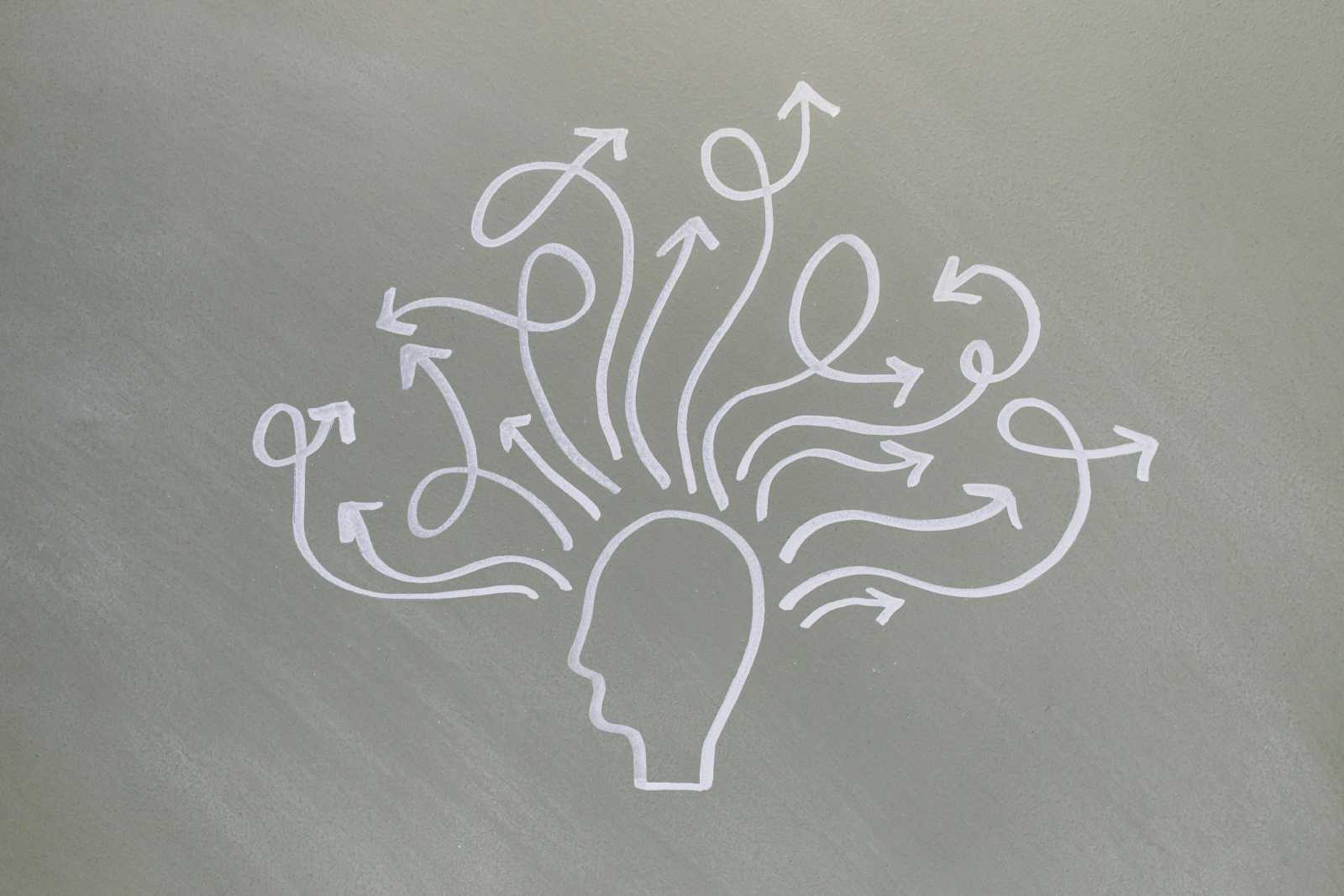
विज्ञान की सीमाएँ
आज की क्वांटम भौतिकी भी तर्क की सीमाएँ दिखा रही है। डबल-स्लिट प्रयोग में इलेक्ट्रॉन एक साथ कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तार्किक रूप से यह असंभव है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से सत्य है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी मानते थे कि तर्क की एक सीमा है, जिसके आगे केवल अनुभव और अंतर्दृष्टि काम करती है।
इसी तरह, बुद्ध की कई बातें तार्किक दिमाग को हजम नहीं होतीं। जैसे— “निर्वाण (जो अ-रचित है) तक पहुँचने के लिए अष्टांगिक मार्ग (जो रचित है) कैसे मदद कर सकता है?” बुद्ध ने इसे कार्य-कारणता के नियम से समझाया। यह गणित के उस नियम जैसा है जहाँ किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम ‘अनंत’ (Infinity) आता है। इसमें कोई ठोस तर्क नहीं होता, बस उस सिद्धांत को स्वीकार करना होता है क्योंकि वह काम करता है।
कुछ विशिष्ट प्रकार की ऊँची समाधि हमें वहाँ ले जाती है जहाँ मन अचानक ‘वर्णन-रहित’ हो जाता है। हर चीज़ परिभाषा से परे हो जाती है। यदि आप इसे केवल तर्क से देखें तो यह बेतुका लग सकता है, परंतु यह वाकई काम करता है।

सुरक्षित दांव
अंततः, बुद्ध उन अति-तार्किक लोगों को, जो हर चीज़ में प्रमाण मांगते हैं, एक ‘सुरक्षित दांव’ खेलने की सलाह देते हैं (अपण्णक सुत्त)। वे कहते हैं कि मान लो, तुम्हें पक्का नहीं पता कि पुनर्जन्म या कर्मफल सच है या झूठ। फिर भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए:
(१) यदि मैं दुराचारी बनता हूँ—
- अगर परलोक नहीं है: तब भी इस जीवन में समाज मेरी निंदा करेगा, मुझे अपयश मिलेगा और मैं कानून के डर में जिऊंगा। (वर्तमान में हानि)
- अगर परलोक है: तो मरने के बाद दुर्गति/नरक मिलेगा। (भविष्य में हानि)
- परिणाम: दोनों दांव उल्टे पड़े। यानी पूर्ण घाटा।
(२) यदि मैं सदाचारी बनता हूँ—
- अगर परलोक नहीं है: तब भी इस जीवन में मुझे सम्मान, प्रेम और मानसिक शांति मिलेगी। लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। (वर्तमान में लाभ)
- अगर परलोक है: तो मरने के बाद सुगति/स्वर्ग मिलेगा। (भविष्य में लाभ)
- परिणाम: दोनों दांव सही पड़े। यानी पूर्ण जीत।
इस तरह, बुद्ध अति-तार्किक व्यक्ति को एक सुरक्षित दांव खेलने की सलाह देते हैं—यदि कर्म और परलोक झूठ भी हों, तब भी सदाचार लाभ देता है; और यदि सच हों, तब तो और भी।
प्रश्न यह नहीं कि कोई बात कितनी तार्किक है। प्रश्न यह है कि वह हमारे भीतर क्या कर रही है। जो विचार अहं बढ़ाए, दूसरों को तुच्छ बनाए या चित्त को कठोर करे—वहाँ विवेक नहीं है। और जो अभ्यास चित्त को कोमल, स्पष्ट और मुक्त करे—वही उसकी सबसे बड़ी कसौटी है।
अंत में, तर्क एक मानचित्र (Map) की तरह है, और विवेक उस यात्रा पर चलने के साहस की तरह। मानचित्र जरूरी है, लेकिन केवल मानचित्र को घूरने से यात्रा पूरी नहीं होती। बुद्ध का धर्म तर्क के नक़्शे में उलझना नहीं, बल्कि विवेक के साथ उस मार्ग पर चलना है। क्योंकि अंततः प्यास पानी का रासायनिक सूत्र (H₂O) रटने से नहीं, बल्कि पानी पीने से बुझती है।