अत्त
|
अतम्मयता
|
अनत्त
|
अभिधम्म
|
अरहं
|
अरिय
|
अनागामी
|
अनुसय
|
अरूप
|
आचरिय
|
आनेञ्ज
|
आपत्ति
|
आसव
|
इदप्पच्चयता
|
उपज्झाय
|
उपधि
|
उपसंपदा
|
उपादान
|
उपोसथ
|
ओतप्प
|
कम्म
|
कम्मट्ठान
|
किलेस
|
खन्ध
|
गन्धब्ब
|
चक्कवाळ
|
छन्द
|
झान
|
तथागत
|
देव
|
धुतङ्ग
|
धम्म
|
धम्मानुसारी
|
नाग
|
नाम-रूप
|
नीवरण
|
निब्बाण
|
पच्चेकबुद्ध
|
पञ्ञा
|
पटिच्चसमुप्पाद
|
पपञ्च
|
पब्बज्जा
|
पवारणा
|
परिब्बाजक
|
पारमि
|
पेत
|
बोधिपक्खिय
|
ब्रह्मचरिय
|
ब्रह्मविहार
|
ब्रह्मा
|
ब्राह्मण
|
भगवा
|
भव
|
भिक्खु
|
मण्डल
|
मार
|
मोह
|
यक्ष
|
राग
|
रूप
|
लोकधम्म
|
लोकधातु
|
वेदना
|
विञ्ञाण
|
विनय
|
विपस्सना
|
विभज्जवाद
|
सकदागामी
|
सञ्ञा
|
सद्धानुसारी
|
समण
|
समथ
|
सम-विसम
|
समाधि
|
सम्मा-सम्बुद्ध
|
सङ्खार
|
सामणेर
|
सेक्ख
|
संवेग
|
संसार
|
संयोजन
|
सोतापन्न
|
सुमेरु
|
हिरी
|
३१ लोक
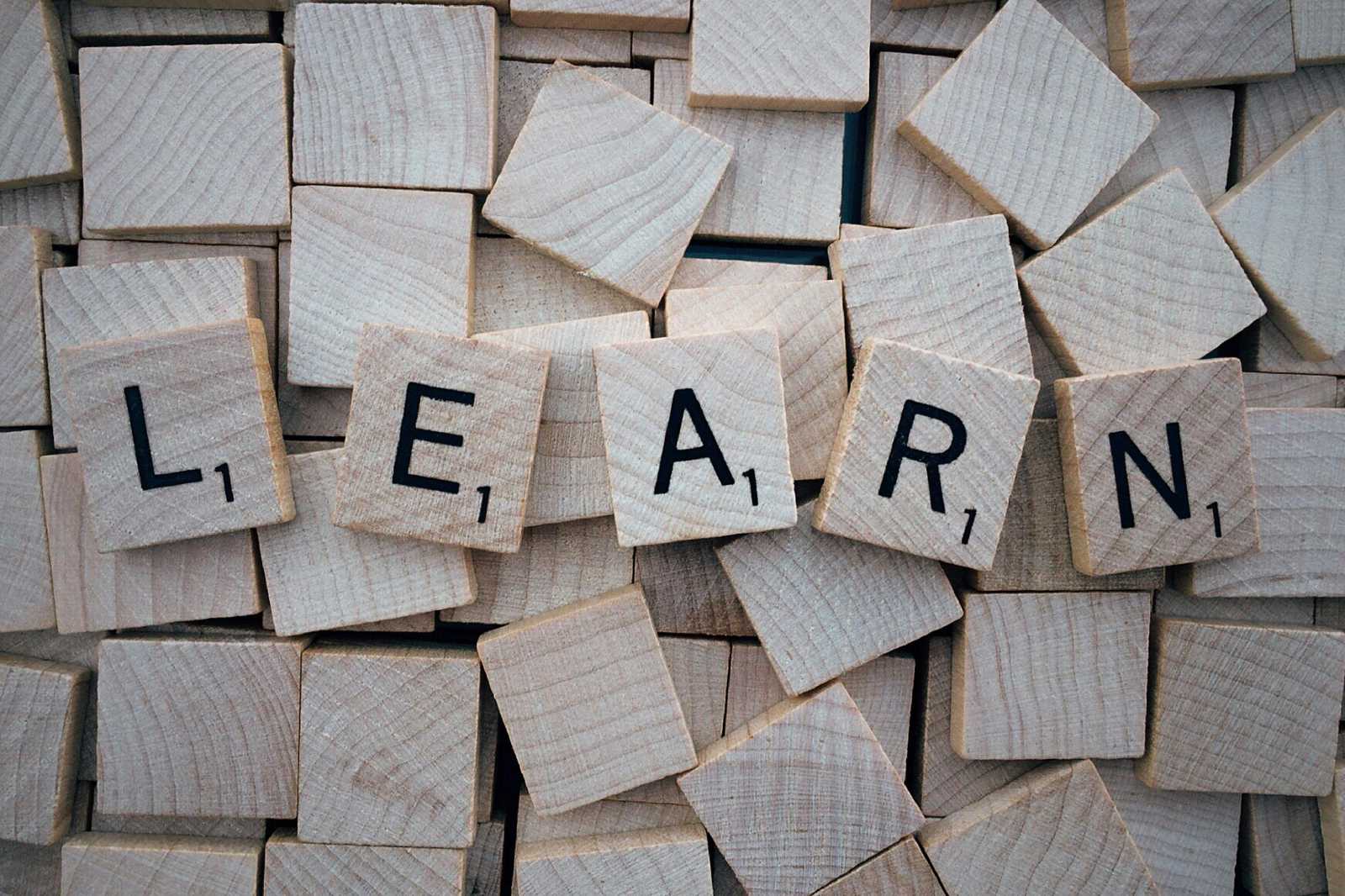
बौद्ध शब्दावली
भगवान बुद्ध ने सिखाया कि धम्म को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए—झूठी प्रशंसा या अलंकरण की कोई ज़रूरत नहीं। धम्म का उद्देश्य है दुःख से मुक्ति, न कि उसे काव्यात्मक या आकर्षक बनाकर प्रशंसा बटोरना। यदि कोई धम्म की झूठी निंदा या तारीफ करता है, तो साफ़ और सीधे बता देना चाहिए—‘इस धम्म में ऐसा नहीं है।’
बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग एक हजार वर्षों बाद, कुछ भाषाविद भिक्षुओं ने धम्म-विनय के अनेक पहलुओं को जटिल और गूढ़ बनाते हुए उसे एक नया रूप दे दिया। जिन मुद्दों पर बुद्ध मौन रहे थे, उन्हें तर्कों और नई धारणाओं से भरने का प्रयास किया। इसने लोगों को धम्म की सहज स्पष्टता से दूर कर दिया और मुक्ति के मूल उद्देश्य से भटकाव पैदा किया। ऐसे प्रयासों ने धम्म को विशेष और श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में साधकों को मिथ्या दृष्टियों में उलझा दिया।
यह भी समझना ज़रूरी है कि यह धम्म किसी अन्य धम्म के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है—न तो सुंदरता, गहराई, या विशिष्टता के मामले में। इसकी वास्तविक प्रतिस्पर्धा अज्ञानता से है। धम्म का उद्देश्य मुक्ति का मार्ग दिखाना है, न कि दूसरों से श्रेष्ठता सिद्ध करना। धम्म की वास्तविक सुंदरता उसकी सादगी और स्पष्टता में है। हमारा प्रयास है कि धम्म को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए—भले ही वह गहरा लगे या सतही, लेकिन सटीक और सच्चा हो।
भगवा / भगवान / भगवत
‘भगवा’ का सीधा अर्थ है ‘धन्य’, ‘पवित्र’, और ‘पूजनीय’।
यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था, जो किसी धम्म-समुदाय में सबसे अधिक पूजनीय हो। पालि शब्द ‘भग’ का संबंध ‘भाग्य’ और ‘भाग’ से भी है, जिससे ‘भगवा’ का एक अर्थ ‘भाग्यवान’ या ‘सौभाग्यशाली’ भी निकलता है—वह व्यक्ति जो अपने महान कर्मों के कारण भाग्यशाली हुआ हो।
एक अन्य दृष्टिकोण से, ‘भाग’ का अर्थ है ‘विभाजन’ या ‘साझा करने वाला’, जिससे ‘स्वामी’, ‘प्रभु’, या ‘मालिक’ का भी बोध होता है। इसे अंग्रेजी में ‘Lord’ कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा धम्म-संपन्न व्यक्ति, जिसने करुणावश अपने धम्म का जनता में विभाजन और वितरण किया हो, वही ‘भगवा’ कहलाता है। इस तरह, उसकी उदारता और ज्ञान से जनता भी धन्य और धम्म-संपन्न हुई।
सैकड़ों वर्षों बाद, कुछ भाषाविद भिक्षुओं ने ‘भगवा’ शब्द की व्याख्या में बदलाव किया। उन्होंने इसे काव्यात्मक रूप में परिभाषित करते हुए ‘भग’ को ‘भग्ग’ से जोड़ा, और कहा कि ‘जो व्यक्ति अपने भीतर के राग , द्वेष, और मोह को भग्न करता (तोड़ देता) है, वही ‘भगवान’ है।’ हालांकि, यह व्याख्या संदिग्ध और अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस तरह की परिभाषा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर यह परिभाषा मान्य होती, तो ‘भगवान’ शब्द अर्हत शिष्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता।
वास्तव में, ‘भगवान’ शब्द का उपयोग बुद्ध से पहले भी होता आ रहा था। श्रमण परंपरा में जैन गुरु महावीर और अन्य समकालीन गुरुओं के लिए, ब्राह्मण परंपरा में ब्रह्मा और देवताओं के लिए, और बाद में विष्णु के अवतारों के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया गया। हाल ही में, ओशो और नेपाली गुरु धम्म संघ जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के लिए भी ‘भगवान’ शब्द का प्रयोग हुआ है।
तथागत
तथागत का अर्थ (तथ+आगत) है, अर्थात, “जो वास्तविकता पर आ गया”। अथवा (तथा+गत) है, “जो वास्तव में पार चला गया” ।
यह शब्द बुद्ध द्वारा नहीं गढ़ा गया था; यह पहले से प्रचलित था। उस समय के लोग इसे ऐसे दुर्लभ व्यक्ति के लिए प्रयोग करते थे, जिसने इसी जीवन में सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो और जिसके लिए कोई अगली मंजिल न बची हो।
बुद्ध ने अक्सर इस शब्द का प्रयोग अपने लिए किया। हालाँकि, बौद्ध परंपरा में यह शब्द विशेष रूप से बुद्ध के लिए ही प्रयुक्त होता है। फिर भी, भगवान कभी-कभी ‘तथागत’ शब्द को अपने अन्य अरहंत शिष्यों के लिए भी इस्तेमाल करते थे।
सम्मा-सम्बुद्ध / सम्यक-सम्बुद्ध
‘सम्मा’ का अर्थ है सम्यक, सही, सटीक, ठीक, यथायोग्य। और ‘सम्बुद्ध’ का अर्थ है, जिसे ‘संबोधि’ प्राप्त हो। इस पर हमारा लेख पढ़ें 👉 संबोधि क्या है?
कई प्राचीन सूत्रों में यह उल्लेख मिलता है कि यह शब्द पहले से प्रचलित था, हालांकि किसी भी श्रमण या ब्राह्मण ने इसे अपने लिए नहीं अपनाया था। सिद्धार्थ गौतम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया।
हालांकि प्राचीन बौद्ध साहित्य में ‘संबोधि’ का एक ही प्रकार माना जाता था। भगवान ने कई सूत्रों में स्पष्ट किया है कि उनके शिष्यों की बोधि और उनकी बोधि में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने केवल प्रथम चार आर्यसत्य की खोज कर संबोधि पहले प्राप्त की और धम्मचक्र प्रवर्तन कर उस मार्ग को प्रदर्शित किया, इसलिए उन्हें ‘सम्मा-सम्बुद्ध’ कहा जाता है।
लेकिन सैकड़ों वर्षों बाद, महायान अवधारणाओं के उदय के साथ, संबोधि की तीन संकल्पनाएं प्रचलित हुईं—
- सम्मा-संबोधि,
- प्रत्येक-बोधि,
- श्रावक-बोधि।
कहा गया कि प्रत्येक-बोधि 'प्रत्येक-बुद्ध' को, और श्रावक-बोधि बुद्ध के अरहंत शिष्य को मिलती है। इन तीनों में पारमिताओं का अंतर बताया गया, जबकि इसका प्राचीन सूत्रों में कोई उल्लेख नहीं मिलता।
इसके साथ ही बोधिसत्व-शपथ और भविष्य के बुद्धत्व की कल्पना प्रमुख हो गई, और तत्काल दुःख-निरोध का मार्ग पृष्ठभूमि में चला गया। एक ही संबोधि को स्तरों में बाँटने से साधना की मूल दिशा ही बदल गई। इसी संदर्भ को हास्य के साथ समझने के लिए देखें 👉 ➗ अरहंत बनाम बोधिसत्व
पच्चेकबुद्ध / प्रत्येक-बुद्ध
पच्चेकबुद्ध का अर्थ है—अकेले बुद्ध। प्रत्येकबुद्ध वे होते हैं जो बिना किसी गुरु या उपदेश के, अपने ही प्रयास से आर्यसत्यों का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से विमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्रज्ञा स्वयंसिद्ध होती है; वे किसी से सीखी हुई नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न होती है। इस अर्थ में वे भी बुद्ध ही होते हैं—अविद्या, तृष्णा और भव से पूर्णतः मुक्त।
किन्तु प्रत्येकबुद्ध और सम्यक-सम्बुद्ध में एक मूल अंतर है। प्रत्येकबुद्ध धम्मचक्र का प्रवर्तन नहीं करते। अर्थात वे धम्म का सार्वजनिक उपदेश नहीं देते, न ही संघ की स्थापना करते हैं। वे प्रायः एकांत में विचरण करते हैं, कभी अल्पमात्र शिष्यों के साथ, तो कभी पूर्णतः अकेले। उनकी करुणा मौन होती है। वे स्वयं मुक्त होते हैं, पर लोक के लिए व्यवस्थित मुक्तिमार्ग नहीं खोलते।
फिर भी, प्रत्येकबुद्ध इस संसार के लिए महापुण्यक्षेत्र माने जाते हैं। उनका दर्शन, संगति या सेवा अत्यंत पुण्यकारी होती है। जैसे, (संयुत्तनिकाय ३:१९, ३:२० में) “तगरसिखी” नामक प्रत्येकबुद्ध को भिक्षा दिलवाने पर एक व्यक्ति सात जन्मों तक सद्गति पाकर शक्तिशाली देवता बनता है, और उसी कर्म के शेष बचे प्रभाव से श्रावस्ती में सात बात धन्नासेठ श्रेष्ठी बनता है।
कहते हैं कि प्रत्येकबुद्ध ऐसे कालों में प्रकट होते हैं जब समा-सम्बुद्ध का धम्म इस संसार में उपलब्ध नहीं होता। तब भी भगवान बुद्ध इसिगिलि सुत्त में सैकड़ों प्रत्येक-बुद्धों का नाम लेकर किर्तिगाथा कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येकबुद्ध मौन प्रज्ञा, एकांत विमुक्ति और आत्म-साक्षात्कार की चरम संभावना का प्रतीक हैं, जो बिना उपदेश दिए भी धम्म की गरिमा को स्थापित करते हैं।
अरिय / आर्य
इस शब्द का बौद्ध परंपरा में अर्थ हैं “श्रेष्ठ!” अर्थात, ऐसी बात—जो साधारण न हो, जनसामान्य की श्रेणी में न आए। बल्कि जो ख़ास हो, विशिष्ट हो, भिन्न हो। जो ऊँची श्रेणी की हो, अगले स्तर की हो। जो सभ्य हो, भद्र हो, महान हो। जिसके मानक, जिसकी गरिमा और प्रतिष्ठा बहुत ऊँची हो। जो सभी के लिए आदर्शपूर्ण हो, सम्मान और आदर के पात्र हो।
उदाहरण के तौर पर, बुद्ध ने ‘आर्य’ शब्द को अपने चार सत्य के साथ जोड़ा। क्योंकि दुनिया के अनेक सत्य हैं, किन्तु कोई सत्य ऐसा नहीं हैं जिसे जानते ही जन्मों-जन्मों के दुःख खत्म होना शुरू हो जाएँ। जिसका साक्षात्कार होते ही परममुक्ति मिल जाएँ। बल्कि वे चार ही ऐसे सत्य हैं, जिनमें जन्म-मरण की शृंखला तोड़कर तत्काल अमृत चखाने की क्षमता हैं। इसलिए उन्हें साधारण श्रेणी के ‘सत्य’ कहना उचित नहीं हैं, बल्कि ‘आर्य सत्य’ कहना योग्य हैं।
इसी तरह, बुद्ध ने ‘आर्य’ शब्द को संघ के साथ जोड़ा। क्योंकि दुनिया में अनेक संघ हैं, किन्तु कोई संघ ऐसा नहीं हैं, जिनमें दुनिया के श्रेष्ठतम आठ प्रकार के आर्य व्यक्ति मिलते हो— श्रोतापन्न , सकृदागामी , अनागामी , अरहंत , और इनके चार मार्गगामी। इसी तरह, बुद्ध ने आर्य विशेषण को कई ख़ास जगह उपयोग किया हैं।
किन्तु यह शब्द वंशवाद से जुड़ने के कारण विवादास्पद हो गया है। कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं, ऐसा व्यक्ति, जो असाधारण तरह से रूपवान दिखता हो, जिसकी ऊँची कदकाठी हो, गोरी त्वचा हो, नीली आँखें हो, सीधी नाक हो। जैसे, जब भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर-पश्चिमी दिशा से लोग आने लगे, तो वे स्थानीय लोगों की तुलना में भिन्न दिखते थे, और उनके तौर-तरीके भी भिन्न थे। वे स्वयं को आर्य कहते थे, जबकि स्थानीय लोगों को अनार्य (=असभ्य)।
पिछली शताब्दी में एडोल्फ हिटलर ने इसी शब्द का प्रयोग कर जर्मनी की सत्ता छीनी, दुनिया पर राज करने की मंशा से विश्वयुद्ध छेड़ा और लाखों लोग मारे गए। जाहिर हैं, आज इस शब्द का प्रयोग होते ही जानकार लोगों के शरीर में सिरहन दौड़ती हैं।
ब्रह्मचरिय
ब्रह्मचर्य का पारंपरिक अर्थ था—संयमित और शुद्ध जीवन, विशेष रूप से यौन संयम, ब्रह्मा के आचरण से प्रभावित, जैसा कि वैदिक परंपरा में देखा गया। परंतु बुद्ध ने इस शब्द को एक नई गहराई दी। उन्होंने इसे केवल संयम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ‘सम्पूर्ण शुद्धि’ और ‘अंतिम मुक्ति’ के रूप में परिभाषित किया। अर्थात, “ब्रह्मचर्य परिपूर्ण तब होता है जब वह निर्वाण पर समाप्त हो।” यानी यह कोई व्रत या जीने की कला नहीं, बल्कि संपूर्ण दुख-मुक्ति का मार्ग है।
बुद्ध और उनके अरहंत शिष्य निर्वाण प्राप्त करने पर घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह ब्रह्मचर्य जीवन न केवल आरंभ किया, बल्कि “पूरा कर लिया”, “जी लिया”, और अंततः “उसे पार कर” निर्वाण तक पहुँचे। यही कारण है कि वे अपने बारे में कहते हैं: “ब्रह्मचर्य समाप्त हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, अब कोई पुनर्जन्म नहीं।” इस प्रकार, ब्रह्मचर्य उनके धम्म में केवल यौन ‘संयम’ नहीं, बल्कि अंतिम सच्चाई तक पहुँचने का मार्ग है।
धम्म / धर्म / स्वभाव
‘धम्म’ या ‘धर्म’ के अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। जैसे, विश्वव्यापी सत्य, अस्तित्व की वास्तविकता, विधि का विधान, सृष्टि का न्याय, आध्यात्मिक मार्ग, प्रवचन, मन का स्वभाव, गुण या घटना, चित्त की प्रवृत्ति, विज्ञान का झुकाव, दार्शनिक सिद्धांत, जीवन के उसूल, जीने की कला, आदर्श नैतिकता, और आचार-सदाचार।
भगवान के धम्मगुणों को इस तरह बताया जाता है:
‘वाकई भगवान का धम्म—स्पष्ट बताया है, तुरंत दिखता है, कालातीत है, आजमाने योग्य, परे ले जाने वाला, समझदार द्वारा अनुभव योग्य!’
हालांकि पिछली शताब्दी के विद्वानों ने ‘धम्म’ और ‘धम्म’ शब्द में ख़ासा अंतर बताने की कोशिश की। उन्होंने धम्म को हिन्दू ‘संप्रदाय’ से जोड़ा, और धम्म को बुद्ध की सीख से। लेकिन दरअसल इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है, जिसे सीमित करने से बुद्ध की सीख ही सीमित हो जाती है।
बुद्ध ने अपनी मुक्ति की सच्चाई को ‘धम्म’ कहा। उन्होंने देव-मानवों को मार्ग दिखाने और सिद्धांत सिखाने को भी ‘धम्म’ का नाम दिया। किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, और वृत्ति को भी ‘धम्म’ कहा गया, और उसके मन में प्रकट होने वाली बातों को भी इसी नाम से संबोधित किया गया। किसी अन्य गुरु की सीख और मार्ग को भी ‘धम्म’ माना गया।
अभिधम्म
“अभिधम्म” का अर्थ है—“ऊँचा या गहरा धम्म”। प्रारंभिक सूत्रों में, जैसे मज्झिमनिकाय १०३ , यह शब्द किसी अलग “पिटक” के लिए नहीं, बल्कि बिलकुल स्पष्ट रूप से ३७ बोधिपक्खिय धम्म के लिए उपयोग होता है।
इन सूत्रों में “अभिधम्म” का प्रयोग “अभिविनय” के साथ—“अभिधम्म–अभिविनय”—मिलता है। यह भी स्पष्ट करता है कि अभिधम्म उस समय कोई पृथक पिटक नहीं था, बल्कि धम्म और विनय की गहरी और ऊँची अभिव्यक्ति का संकेत था।
ऐतिहासिक रूप से, अभिधम्म का एक स्वतंत्र पिटक के रूप में उभरना अशोक-काल की तृतीय भिक्षु-संगीति (ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी) से जुड़ा है। इसी संदर्भ में भिक्षु मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा कथावत्थु की रचना हुई, जो संघ में उत्पन्न मतभेदों के खंडन हेतु रचा गया एक उत्तरवर्ती ग्रंथ है। बाद में थेरवाद परंपरा में अभिधम्म को सात ग्रंथों सहित एक स्वतंत्र पिटक का स्थान दिया गया, जिसमें धम्म को विश्लेषणात्मक ढंग से वर्गीकृत किया गया—जैसे चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान ।
परंतु प्रारंभिक सूत्रों के आलोक में यह स्पष्ट है कि बुद्ध द्वारा सिखाया गया “अभिधम्म” वस्तुतः ३७ बोधिपक्खिय धम्म की वही साधना है, जिसे विमुक्ति के लिए पर्याप्त बताया गया है। अतः प्रारंभिक सूत्रों EBT के आधार पर अभिधम्म-पिटक को बुद्धवाणी नहीं, बल्कि भिक्षु-संघ की एक उत्तरवर्ती, व्याख्यात्मक परंपरा के रूप में समझना अधिक संगत है—ज्ञानवर्धक अवश्य, पर मूल धम्म का पर्याय नहीं।
बोधिपक्खिय धम्म / बोधिपक्षिक धम्म
बुद्ध ने जीवन भर जो कुछ सिखाया, उसका मूल उद्देश्य था—दुःख से मुक्ति। लेकिन कुछ शिक्षाएँ ऐसी थीं जिन्हें उन्होंने स्वयं निर्वाण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। इन्हीं को कहा गया बोधिपक्खिय धम्म—अर्थात वे ३७ विशेष धम्म जो बोधि के पक्ष में सहायक हैं, मानो बोधि के पंख हों।
बोधिपक्खिय धम्म केवल ज्ञान, कौतूहल या बौद्धिक चर्चा के विषय नहीं हैं, बल्कि सीधी साधना की ठोस राह हैं। ये वे धार्मिक गुण हैं जिन्हें भीतर विकसित करने से साधक मुक्तिपथ पर आगे बढ़ता है।
बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में बार-बार यही कहा—जब तक ये शिक्षाएँ स्मरण में रहेंगी और आचरण में जीवित रहेंगी, तब तक बुद्धसासन जीवित रहेगा—
भिक्षुओं, मैंने ये धम्म तुम्हें प्रत्यक्ष-ज्ञान से बताए हैं, उन्हें भली प्रकार सीखना, धारण करना, विकसित करना, बार-बार कर के बढ़ाना, ताकि ये ब्रह्मचर्य मार्ग चिरस्थायी बना रहे—बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, इस दुनिया पर उपकार करते हुए, देव और मानव के कल्याण, हित और सुख के लिए! कौन-से धम्म?
हालाँकि बुद्ध ने खुद इन ३७ शिक्षाओं को कभी “बोधिपक्खिय धम्म” नहीं कहा, शुरूआती सुत्तों में उन्होंने केवल ‘सात बोध्यङ्ग’ को, तो कभी ‘पाँच इंद्रियों’ को ही इस नाम से संबोधित किया। लेकिन बाद में संयुक्तनिकाय में इन्हें एक संगठित समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया, और कालांतर में इसी रूप में स्वीकार भी किया गया।
बोधिपक्खिय धम्म बुद्ध की साधना का सार हैं। मुक्ति का मार्ग इन्हीं ३७ तत्वों पर टिका है। और जब तक ये टिके रहेंगे, बुद्ध का धम्म भी जीवित रहेगा।
इनकी साधना करने का तरीका पढ़ें ३७ बोधिपक्खिय धम्म
पारमि / पारमिता
पारमि शब्द ‘परम’ से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ है किसी धम्म-गुण को साधना द्वारा उसकी “परम अवस्था” तक विकसित करना।
आज थेरवाद परंपरा में प्रचलित रूप से दस पारमियाँ मानी जाती हैं—दान, शील, निष्काम, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, सच्चाई, अधिष्ठान, मेत्ता और उपेक्षा—और इनके तीन स्तर बताए जाते हैं:
- पारमि — सामान्य दान या अन्य गुणों का अभ्यास और विकास।
- उप-पारमि — कठिन तप, संयम और त्याग के माध्यम से की गई परिपूर्णता।
- परमत्थ-पारमि — जहाँ साधक अपनी पारमि की पूर्ति के लिए प्राण तक दाँव पर लगाने को तैयार होता है।
यद्यपि ‘पारमि’ बौद्ध परंपरा में एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरक अवधारणा है, फिर भी प्रारंभिक बौद्ध सूत्रों EBT में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका व्यवस्थित रूप महायान परंपरा के साथ उभरता है, जहाँ इसे “बोधिसत्व आदर्श” के अंतर्गत, अनेक जन्मों या कल्पों तक गुण-संचय की दीर्घ प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया।
यह मार्ग सुनने में सुंदर और प्रेरणादायक अवश्य लगता है, पर मूल बुद्धवचन की कसौटी पर यह संभावित मिथ्या-दृष्टि की श्रेणी में आ सकता है। इसका कारण यह है कि यहाँ मुक्ति को भविष्य के किसी लक्ष्य पर टाल दिया जाता है—जहाँ व्यक्ति स्वयं को “बोधिसत्व” मानकर जन्म-जन्मांतर तक पुण्य और गुण इकट्ठा करता रहता है, बजाय इसके कि इसी जीवन में दुःख की निरोध का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करे।
इस विषय पर हमारा हास्य-लेख भी देखें 👉 अर्हंत या बोधिसत्व?
इसलिए, पारमि की अवधारणा प्रेरक और उपयोगी होते हुए भी मूल बुद्धवचन के अनुसार न तो आवश्यक है और न ही अनिवार्य। कुछ साधकों के लिए यह अनजाने में अहंकार और भव-तृष्णा का आधार भी बन सकती है।
इस विषय को और गहराई से समझने के लिए पढ़ें 👉 पारमिता का मिथक
कम्मट्ठान / कर्मष्ठान
‘कम्मट्ठान’, ‘कर्मष्ठान’, या ‘कर्मस्थान’ का मूल अर्थ है—आजीविका कमाने के लिए कार्य या उसका आधार।
प्रारंभिक सूत्रों में यह शब्द सामान्यतः किसी के जीविकोपार्जन के माध्यम, जैसे कि खेती, कुम्हारी, शिल्प-कला या व्यवसाय के लिए प्रयुक्त होता है। जिस कार्य से कोई व्यक्ति जीवन-निर्वाह करता है, वही उसका ‘कम्मट्ठान’ कहलाता है।
उदाहरण के लिए, अंगुत्तरनिकाय (८:५४, ८:५५, ८:७६, १०:४६ आदि) में भगवान उपासकों से कहते हैं, “जिस कर्मष्ठान से तुम आजीविका कमाते हो…"। सुभ सुत्त में, भगवान गृहस्थों के “घरावास-कम्मट्ठान” और भिक्षुओं के “पब्बज्जा-कम्मट्ठान” (भिक्षुओं के सङ्घिक कार्य) के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। इस सन्दर्भ में भी ‘कम्मट्ठान’ का आशय आजीविका कार्य के स्वरूप और उसके उद्देश्य से है, न कि ध्यानविधियों से।
सुत्तपिटक के किसी भी स्थान पर भगवान ने किसी साधना-पद्धति या ध्यान-अभ्यास को कभी ‘कम्मट्ठान’ नहीं कहा। न तो आनापानसति , न ब्रह्मविहार , न असुभ , और न ही अन्य ध्यानविधियों को कभी इस शब्द से संबोधित किया गया।
किन्तु लगभग एक सहस्राब्दी बाद, आचार्य बुद्धघोष ने जब विसुद्धिमग्ग की रचना की, तब उन्होंने ‘कम्मट्ठान’ शब्द को पुनर्परिभाषित किया। अब यह शब्द ध्यान-साधना के विषयों के लिए प्रयुक्त होने लगा। उन्होंने १० कसिण, १० असुभ , १० अनुस्सति, ४ ब्रह्मविहार, ४ अरूप समापत्तियाँ , आहार प्रतिकूल संज्ञा , और चार धातु व्यवस्थान को मिलाकर ४० ध्यान विषयों को ‘कम्मट्ठान’ कहा।
हालाँकि, जब हम प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में भगवान द्वारा प्रतिपादित ध्यानविधियों का संकलन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि केवल ४० नहीं, अपितु कम से कम ५२ ध्यान विषयों का निर्देश स्वयं बुद्ध ने विभिन्न सुत्तों में किया है—जिनमें अनेक प्रकार की संज्ञाएँ (जैसे: अनित्य संज्ञा , विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, आदीनव संज्ञा , सब्बलोके अनभिरति संज्ञा इत्यादि) और विभिन्न तरह के ध्यान शामिल हैं।
विभज्जवाद
“विभज्जवाद” का सीधा आशय है—“विभाजित करके अलग-अलग बताना।” इसे समझने के लिए पञ्ह-कोसल्ल, अर्थात “प्रश्न-निपुणता”, को समझना आवश्यक है। वह कौशल जिसके आधार पर कोई जानता है कि किस प्रकार के प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर दिया जाना चाहिए।
अंगुत्तरनिकाय ४:४२ (पञ्हब्याकरण सुत्त) में भगवान बताते हैं कि किसी समझदार व्यक्ति को प्रश्न सुनकर उनका वर्गीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। वे प्रश्नों को चार श्रेणियों में विभाजित करते हैं—
- एकंस-ब्याकरणीयो: जिनका उत्तर सीधे ‘हाँ’ या ‘ना’ में दिया जा सकता है।
- विभज्ज-ब्याकरणीयो: जिनका उत्तर सीधा ‘हाँ’/‘ना’ में देना उचित नहीं होता; ऐसे प्रश्न पहले विभाजित और परिभाषित किए जाते हैं, फिर अलग-अलग संदर्भ में उनका उत्तर दिया जाता है।
- पटिपुच्छा-ब्याकरणीयो: जिनके उत्तर में प्रश्नकर्ता की दृष्टि को खोलने हेतु प्रतिप्रश्न किया जाता है।
- ठपनियो: जिन्हें अनुत्तरित छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कल्याणकारी मूल्य नहीं होता और वे केवल मिथ्यादृष्टि को बढ़ावा देते हैं।
बाद के कालों में इस शब्द को उसके मूल संदर्भ से हटाकर इस प्रकार इस्तेमाल किया गया कि स्वयं संघ के भीतर भी “विभज्जवाद” को एक पंथ-सूचक शब्द बना दिया गया। आगे चलकर कहा जाने लगा कि बुद्ध स्वयं विभज्जवादी थे, और “सच्चा” भिक्षुसंघ वही है जो विभज्जवादी है। श्रीलंकाई थेरवाद को भी इसी विभज्जवाद की परम्परा में रखा गया, जहाँ धम्म के पहलुओं को कई बार अनावश्यक रूप से अति-विश्लेषण कर अभिधम्म के चश्मे से समझना प्रमुख माना जाता है।
जबकि वास्तव में, भगवान ने परिस्थिति के अनुसार सभी चार पद्धतियाँ अपनाईं थी—कभी सीधे उत्तर दिए, कभी विभाजित करके, कभी प्रतिप्रश्न से, और कभी मौन रखकर भी।
इसी प्रवाह में अट्ठकथाओं और अन्य पालि साहित्य की उत्पत्ति हुई, जो अनेक बार भगवान के मूल वचन से भटककर धम्म के प्राथमिक संदर्भ को समझने में बाधा भी बन गई। ध्यान देने की बात है कि “विभज्जवाद” केवल बौद्ध परंपरा का शब्द नहीं; यह जैन साहित्य में भी मिलता है (सूयगड १४.२२)।
राग
‘राग’ का सामान्य अर्थ हम अक्सर आकर्षण, खिंचाव, या किसी विषय में गहरी दिलचस्पी से लगाते हैं। किन्तु धम्म में इसका शाब्दिक और सटीक अर्थ है—‘रंग’, ‘रंजन’ या ‘डाई’।
जिस प्रकार एक उज्ज्वल सफ़ेद वस्त्र पर यदि लाल रंग चढ़ जाए, तो वह ‘रंजित’ होकर अपनी मूल उज्ज्वलता खो देता है; ठीक उसी प्रकार जब चित्त किसी विषय या अनुभूति में डूबकर उसी के रंग में रंग जाता है, तो उस आवेशित मानसिक अवस्था को ‘राग’ कहते हैं।
अक्सर लोग ‘राग’ को केवल काम-वासना तक सीमित कर देते हैं, जिसे पालि में ‘काम-राग’ कहा गया है। किन्तु सुत्तों में ‘राग’ का दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। यह स्थूल और सूक्ष्म, दोनों स्तरों पर होता है:
- काम-राग: पाँच इन्द्रियों के सुखों के प्रति तीव्र खिंचाव।
- रूप-राग: रूप के प्रति या रूप अवस्थाओं के प्रति आकर्षण।
- अरूप-राग: अरूप (निराकार) मानसिक उपलब्धियों के प्रति सूक्ष्म आकर्षण।
- भव-राग: ‘मैं हूँ’ और ‘मैं बना रहूँ’—अपने भव (अस्तित्व) को बनाए रखने की यह जद्दोजहद भी राग ही है।
राग की उत्पत्ति किसी वस्तु या अनुभव में ‘आस्वाद’ (मज़ा) देखने से होती है। यह केवल एक साधारण ‘रुचि’ से शुरू होकर आकर्षण में बदलता है, और अंततः चित्त उसमें पूरी तरह गध जाता है। भगवान ने इसीलिए इसे बुखार और आग की उपमा दी है, क्योंकि यह चित्त की शांति को जला देता है।
जहाँ ‘लोभ’ किसी अप्राप्त वस्तु को पकड़ने या निगलने की इच्छा है, वहीं ‘राग’ प्राप्त अनुभव में खींचे जाने, रम जाने, या रंगे जाने की स्थिति है। मुक्ति का मार्ग इसीलिए ‘विराग’ कहलाता है—जिसका अर्थ है रंग का फीका पड़ जाना या उतर जाना। जब चित्त से दिलचस्पी का यह रंग उतर जाता है, तभी वह अपने मूल, शांत स्वभाव में लौटता है।
राग का ठीक विपरीत ‘पटिघ’ है। जहाँ राग किसी अनुभव से खींचा चला जाकर स्वीकार करता है, वहीं ‘पटिघ’ उसे नकारता है, धकेलता है, टकराता है, घर्षण या प्रतिरोध करता है।
मोह
‘मोह’ का शाब्दिक अर्थ है—‘मूढ़ता’, ‘बेहोशी’, या ‘चित्त का संमोहित हो जाना’। यह केवल ‘जानकारी का अभाव’ नहीं है, बल्कि वास्तविकता को न देख पाने की एक गहरी मानसिक धुंध है।
जिस प्रकार घने कोहरे में साफ़ रास्ता भी दिखाई नहीं देता और व्यक्ति भटक जाता है, उसी प्रकार मोह के कारण चित्त यह भेद नहीं कर पाता कि क्या करने योग्य (कुशल) है और क्या न करने योग्य (अकुशल)। यह प्रज्ञा के अंधापन की वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति सत्य के विपरीत देखता है और बेहोशी में गलत चुनाव करता है।
अक्सर लोक-भाषा में ‘मोह’ को ‘ममता’ या ‘प्रेम’ (जैसे पुत्र-मोह) के अर्थ में बहुत हल्का कर दिया गया है। किन्तु धम्म में यह एक खतरनाक क्लेश (विकार) है। सुत्तों में इसे ‘अविद्या’ की जड़ माना गया है। व्यक्ति किसी विषय पर आकर्षित राग या क्रोधित (द्वेष) तभी होता है, जब वह उस विषय के वास्तविक स्वभाव के प्रति ‘मूढ़’ या ‘बेखबर’ हो।
जब तक मोह का पर्दा पड़ा है, तब तक व्यक्ति अपने ही द्वारा रचे गए भ्रमजाल को सच मानता रहता है। प्रज्ञा (अंतर्ज्ञान) ही एकमात्र प्रकाश है जो इस अंधेरे को चीर सकती है।
छन्द / चाह
‘छन्द’ का अर्थ है—‘इच्छा’, ‘आकांक्षा’, ‘चुनाव’ या ‘किसी कार्य को करने का संकल्प’।
अक्सर इसे तृष्णा समझकर त्यागने की बात की जाती है, जो कि अनुचित है। जहाँ तृष्णा निश्चित तौर पर एक अकुशल मूल है जो भव की ओर ले जाती है, वहीं ‘छन्द’ एक ऐसा चेतसिक है जो नैतिक रूप से तटस्थ है। अर्थात, कोई छन्द कुशल है या अकुशल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है।
- काम-छन्द: इंद्रिय सुखों की कामना (यह पाँच नीवरणों में से एक है, जिसे त्यागा जाना चाहिए)।
- धम्म-छन्द: साधना करने की, सत्य को जानने की, या निर्वाण प्राप्त करने की तीव्र इच्छा (यह आवश्यक है)।
विनयपिटक में इसका उल्लेख ‘सहमति’ या ‘चुनाव’ के संदर्भ में भी आता है; जब संघ किसी विषय पर सामुहिक निर्णय लेता है, तो भिक्षु अपना ‘छन्द’ (मत) देते हैं।
आनन्द भंते ने स्पष्ट किया है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए ‘छन्द’ का होना अनिवार्य है। जैसे किसी दूर के बगीचे तक पहुँचने के लिए ‘इच्छा’ की ज़रूरत होती है, और वहाँ पहुँचने के बाद वह इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है; वैसे ही अरहंत होने तक उस मुक्ति के ‘छन्द’ को विकसित करना होता है। ‘इच्छा-रहित’ होना यात्रा का परिणाम है, मार्ग नहीं।
आसव / आस्रव
आस्रव का सरल अर्थ है—स्त्राव, रिसाव, बहाव, या प्रवाह। यह वह पुराना, सड़ा हुआ मानसिक द्रव्य है, जो समय-समय पर रिसने लगता है। जैसे नाली का गंदा पानी बाहर आने लगे तो आसपास दुर्गंध फैलती है, वैसे ही जब चित्त से आस्रव रिसने लगते हैं, तो शरीर और मन—यानी हमारा आचरण और विचार—दोनों दूषित हो जाते हैं, और वे भी एक प्रकार की ‘बदबू’ देने लगते हैं।
कभी-कभी कोई विशेष ऊर्जा भीतर प्रवाहित होती है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव में चित्त किसी एक दिशा में झुकने लगता है। यही झुकाव आस्रवों के स्त्राव का कारण बनता है। भीतर एक प्रकार की नशा-जैसी स्थिति बनती है, जिससे विशेष प्रकार के स्वभाव, विचार और इच्छाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। इस अवस्था में चित्त जैसे किसी गिरफ्त में आ जाता है, और आगे के सारे कर्म उसी के प्रभाव में किए जाते हैं।
कुछ आस्रव कभी-कभार रिसते हैं, तो कुछ लगातार बहते रहते हैं। अक्सर तीन प्रकार के आस्रव बताएं जाते हैं, लेकिन कभी कभी चार प्रकार के भी आस्रव बताए गए हैं:
- काम-आस्रव – इंद्रिय सुख का प्रवाह
- भव-आस्रव – जीवन, अस्तित्व और सत्ता का प्रवाह
- दृष्टि-आस्रव – धारणाओं और दृष्टिकोणों का प्रवाह
- अविद्या-आस्रव – दुःख के सही कारण के प्रति अज्ञानता का प्रवाह।
भगवान के अनुसार प्रतित्य समुत्पाद की पहली कड़ी “अविद्या”, आस्रव के कारण ही उपजती है, जिससे होकर आगे दुःख की गठरियाँ खुलती है। लेकिन आस्रव का क्षय होने से अविद्या उत्पन्न नहीं होती, और सभी दुःखों से मुक्ति होती है। इसलिए “आस्रवक्षय ज्ञान” ही बौद्ध धम्म का अंतिम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने पर ही कोई निर्वाण का साक्षात्कार कर अरहंत-पद प्राप्त करता है।
भगवान ने सब्बासव सुत्त में सभी प्रकार के आस्रव को समाप्त करने के सात तरीके बताएँ हैं। जैसे, दृष्टि आस्रव को हटाने के लिए योनिसो मनसिकार, और बाकी आस्रव के लिए इंद्रिय संवर, आवश्यकताओं का उचित उपयोग करना, सहन करना, खतरों को टालना, बुराइयों को दूर हटाना, और संबोधि-अंगों की साधना करना शामिल हैं।
अनुसय / अनुशय / अवचेतन
अनुशय का शाब्दिक अर्थ है – ‘सुप्त अवस्था’, या वह जो किसी के साथ सोया हुआ हो। यानी भीतर अवचेतन की गहराई में जमी वे मानसिक प्रवृत्तियाँ, जो तब तक निष्क्रिय या छिपी रहती हैं, जब तक कोई विशेष परिस्थिति उन्हें जगा न दे।
अनुशय गहरे आदतन झुकाव होते हैं, जो समय-समय पर उभरकर व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्मों को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन में ढेर सारे अनुभव, इच्छाएँ और भावनाएँ जमा रहती हैं। व्यक्ति भले ही इन्हें सतह पर न देख पाए, लेकिन जब कोई परिस्थिति इनके अनुकूल होती है, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के भीतर क्रोध का अनुशय दबा हो, तो वह सामान्यतः शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे अपमानित करता है, उसमें क्रोध जागने लगता है। इसी तरह, वासना का अनुशय तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि कोई उत्तेजक दृश्य, स्मृति या अवसर उसे जाग्रत न कर दे।
सात प्रकार के अनुशय होते हैं;
- काम अनुशय – इंद्रिय सुखों की कामुक ललक, जो इच्छा और छन्द (=चाह) के रूप में उभरती है।
- पटिघ अनुशय – चिढ़-चिढ़ होना, क्रोध और आक्रोश की प्रवृत्ति।
- दिट्ठी अनुशय – अपनी ही मान्यताओं को दृढ़ता से पकड़कर रखना, चाहे वे सत्य हों या नहीं।
- विचिकिच्छा अनुशय – समय-समय पर संशय और संदेह की प्रवृत्ति उभरना, जो स्पष्टता को बाधित करती हो।
- मान अनुशय – अहंभाव और दूसरे से तुलना करने की प्रवृत्ति।
- भवराग अनुशय – अस्तित्व की आकांक्षा, जो व्यक्ति को किसी विशेष पहचान, अवस्था या लोक की ओर धकेलती है।
- अविज्जा अनुशय – अज्ञानता की प्रवृत्ति, जो दुख के मूल कारणों को न समझने से उत्पन्न होती है।
किलेस / क्लेश
क्लेष का अर्थ है ऐसे मल, जो चित्त को ढ़क कर हमें और दूसरों को कष्ट देते रहते हैं।
क्लेश मुख्य रूप से तीन होते हैं—लोभ, द्वेष, और मोह। इन तीनों से निकल कर दस प्रकार के क्लेश उपजते हैं। किसी-किसी सूत्र में सोलह भिन्न प्रकार के क्लेशों का उल्लेख हैं—लालच, दुर्भावना, क्रोध, बदले की भावना, अवमानी, अकड़ूपन, ईर्ष्या, कंजूसी, धोखेबाज़ी, डींग हांकना, अहंभाव, घमंड, नशा, लापरवाही, दूसरों को नीचा दिखाना, और अविद्या।
उपधि / उपाधि
उपधि का अर्थ है—वह चीज़ जिससे हम चिपकते हैं, या जो चित्त का बोझ बन जाती है। यह शब्द अक्सर “संपत्ति”, “बोझ”, या “सामग्री” के अर्थ में आता है—लेकिन बौद्ध शिक्षाओं में इसका मतलब है, “आंतरिक मानसिक बोझ”, जिसे चित्त ढोता फिरता है।
सूत्तों में उपधि का संबंध “आसक्ति” और “आत्मग्रहण” से है। यह उन चीज़ों की ओर इशारा करता है जिन्हें व्यक्ति “अपना” मानता है—चाहे वह घर-परिवार या संपत्ति हो। जब चित्त किसी भी चीज़ को “मैं” या “मेरा” कहकर पकड़ लेता है, तो वह उसकी “उपधि” बन जाती है। इसलिए उपधि का सीधा संबंध अपनत्व की भावना से है, जो संसार में बंधन और पुनर्जन्म का कारण बनती है।
चूळनिद्देस (एक अपेक्षाकृत उत्तरकालीन ग्रंथ) में उपधि के दस प्रकार बताए गए हैं: तृष्णा, दृष्टि, क्लेश, कर्म, दुराचरण, आहार (शारीरिक और मानसिक), क्रोध, चार महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु), छह बाह्य इन्द्रिय विषय (रूप, आवाज़, गंध, स्वाद, संस्पर्श, विचार), और छह प्रकार के विज्ञान।
उपादान / आसक्ति
उपादान का अर्थ है—किसी वस्तु को पकड़ना, उस पर टिक जाना, और उसी से मानसिक पोषण लेना। यह केवल चिपकाव नहीं, बल्कि भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव, विचार, दृष्टिकोण या भावना को अपना आधार बना लेती है, जैसे अग्नि किसी ईंधन से चिपकी रहती है और उसी से जलती है।
पालि में उपादान शब्द दो स्तरों पर अर्थ देता है—शारीरिक और मानसिक।
शारीरिक रूप में यह अग्नि के लिए ईंधन और अग्नि की ईंधन को पकड़ने की क्रिया—दोनों को दर्शाता है। मानसिक रूप में यह उस सामग्री को भी दर्शाता है जिससे मन अपने “अस्तित्व” का पोषण करता है, और उस पोषण को पकड़ने की प्रवृत्ति को भी। यही कारण है कि इसे “आश्रय”, “पकड़”, या “जीवित रहने की मनोवृत्ति”—इन सबके रूप में समझा जा सकता है।
प्रथम आर्य सत्य कहता है कि “उपादान ही दुःख है”। यही वह क्रिया है जो अनुभवों को पकड़कर अहंभाव, तृष्णा और भव को जन्म देती है। उपादान के चार प्रकार बताए गए हैं —
- काम उपादान (इन्द्रिय-सुखों की चाह),
- शील-व्रत उपादान (आचार-व्यवहार को आत्म-मुक्ति का साधन मानना),
- दृष्टि उपादान (दृष्टियों, मान्यताओं में जकड़ाव), और
- आत्मवाद उपादान (स्व-अहं की अवधारणाओं में टिकाव)।
ये चार प्रकार के उपादान जब पाँच खन्ध (रूप, वेदना, सञ्ञा, सङ्खार, विञ्ञाण) में जड़ पकड़ लेते हैं, तब वे दुःख का रूप ले लेते हैं। विपस्सना साधना इन्हीं उपादानों को पहचानकर छोड़ने का अभ्यास है। जब चित्त जानता है कि जिसे वह पकड़ रहा है, वही उसका बोझ और दुःख है—तब वह स्वेच्छा से छोड़ने लगता है। यही विमुक्ति की शुरुआत है।
संयोजन / बेड़ी
ऐसी बेड़ियाँ, या ऐसे बन्धन, जो किसी को जन्म-मरण की अनन्त भटकन (=संसरण) में बाँधती हैं।
कुल दस बेड़ियाँ बतायी गयी हैं—
- सक्कायदिट्ठी—स्व-धारणा या आत्म-पहचान की दृष्टि
- विचिकिच्छा—सही-गलत में उलझन, अनिश्चितता, संशय
- सीलब्बत परामासो—कर्मकाण्ड और व्रत में अटकना, रूढ़ि-परंपराओं को धम्म मानना।
- कामराग—कामुकता के प्रति राग (=दिलचस्पी)
- पटिघ—चिड़चिड़ होना, प्रतिरोधी भावना
- रूपराग—भौतिक-रूप में राग
- अरूपराग—अरूपता में राग
- मान—अहंभाव
- उद्धच्च—बेचैनी
- अविज्जा—अविद्या
पहली पाँच बेड़ियों को “निचले पक्ष की बेड़ियाँ” (“ओरम्भागिय संयोजन”) कहते हैं, क्योंकि (संयुक्तनिकाय ४५.१७९, अंगुत्तरनिकाय १०.१३ के अनुसार) वे सत्वों को निचले कामलोक में बांध कर रखते हैं। जबकि अंतिम पाँच बेड़ियों को “ऊँचे पक्ष की बेड़ियाँ (“उद्धम्भागिय संयोजन”) कहते हैं, क्योंकि वे सत्वों को ऊँचे ब्रह्मलोक में बांध कर रखते हैं।
पहली तीन बेड़ियाँ तोड़ने वाले को ‘सोतापन्न’ कहते हैं। चौथी और पाँचवी बेड़ी को दुर्बल करने वाले को ‘सकदागामी’। पहली पाँच बेड़ियाँ तोड़ने वाले को ‘अनागामी’। और सभी दस बेड़ियाँ तोड़ने वाले को ‘अरहंत’।
नीवरण
नीवरण का अर्थ है—मन की वे रुकावटें या आच्छादन, जो चित्त को स्पष्ट देख पाने से रोकते हैं।
ये पाँच मानसिक अवरोध होते हैं, जो समथ और विपश्यना में बाधा उत्पन्न करते हैं। बौद्ध साधना में इनका निरीक्षण और क्षय अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि जब तक चित्त इनसे ढँका रहता है, तब तक वह न तो स्थिर (समथ) हो सकता है, न ही वास्तविकता को ठीक से देख (विपश्यना कर) सकता है।
पाँच नीवरण होते हैं:
- कामच्छन्द—इन्द्रिय-सुखों की कामेच्छा, जो चित्त को बाहर की ओर खींचती है।
- ब्यापाद—दुर्भावना या किसी के प्रति घृणा की भावना, जो चित्त को अशांत करती है।
- थिन-मिद्धा—सुस्ती और तंद्रा।
- उद्धच्च-कुक्कुच्च—बेचैनी और किए गए कर्मों के प्रति पछतावा।
- विचिकिच्छा—संदेह , उलझन या अनिश्चितता।
नीवरणों को दबाना नहीं, पहचान कर त्यागना होता है। जब ध्यान की प्रक्रिया में चित्त इन पाँच आवरणों से मुक्त होता है, तब उसमें प्रकाश, निपुणता और स्थिरता आती है—और वहीं से सच्चे ध्यान और अंतर्दृष्टि की नींव रखी जाती है। पाँच नीवरणों को गहराई से समझने और त्यागने की साधना जानने के लिए हमारी मार्गदर्शिका से यह आवश्यक लेख पढ़ें अकुशल कैसे त्यागें?
निब्बान / निर्वाण
निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है, अग्नि का बुझना, शीतल हो जाना।
अग्नि को जलते रहने के लिए ईंधन या आधार की जरूरत होती है। वह न प्राप्त हो तो अग्नि बुझ जाती या ‘निवृत’ होती है। उसी तरह, किसी सत्व को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पाँच उपादान-स्कन्ध की जरूरत होती है। यदि सर्वस्व उपादान या आधार छूट जाए तो चित्त मुक्त हो जाता है, और इस बुझने की निर्वाणिक अवस्था का साक्षात्कार करता है। वहाँ बेहोशी नहीं होती, बल्कि इंद्रियों से परे परमसुखद ‘नित्य’ का अनुभव होता है।
जिस तरह ईंधन का आधार लेकर कोई ज्वलन प्रक्रिया कष्टदायक, तनावपूर्ण और व्याकुलता से भरी होती है। उसी तरह, पाँच उपादान-स्कंधों का आधार लेकर कोई अस्तित्व प्रक्रिया पीड़ादायक, तनावपूर्ण और व्याकुलता से भरी होती है। भव की प्रक्रिया में लिप्त चित्त को भीतर ही भीतर लगातार पीड़ा, तनाव और ज्वलन महसूस होती है। अथवा वह ईंधन-रूपी आधार छोड़ देने पर अभूतपूर्व शान्ति, राहत और शीतलता महसूस होती है, और साथ ही, समस्त पीड़ा, तनाव और ज्वलन से मुक्ति होती है।
अधिक जानने के लिए पढ़ें: निर्वाण का खौफ़
अत्त / आत्मा
आत्मा को सामान्यतः व्यक्ति का एक शाश्वत, स्थायी और अदृश्य तत्व माना जाता है, जो शरीर और मन से पृथक है। वैदिक, जैन, सिख, ईसाई, इस्लामी तथा अनेक अन्य परंपराओं में इसे अमर, अविनाशी और जन्म–मरण से परे समझा गया है—वह “स्व” या “मैं” की अनुभूति, जिसके साक्षात्कार से परमात्मा को पाने की बात भी कही जाती है।
परंतु भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के प्रश्न को जानबूझकर अनुत्तरित रखा। “आत्मा है” कहना शाश्वतवाद को बढ़ाता, और “आत्मा नहीं है” कहना उच्छेदवाद की ओर ले जाता—दोनों ही अति-दृष्टियाँ मुक्तिपथ में बाधक हैं। इसलिए भगवान ने इस प्रश्न से हटकर साधकों को आसक्ति-त्याग, प्रत्यक्ष-दर्शन, और यथाभूत-ज्ञान की दिशा में अग्रसर किया।
कभी-कभी भगवान आत्मा-संबंधी सकारात्मक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे “अत्ता हि अत्तनो नाथो”—अर्थात “मनुष्य स्वयं का स्वामी है।” यहाँ ‘आत्मा’ का अर्थ किसी स्थायी तत्व से नहीं, बल्कि आत्म-संयम, सजगता, और अपने ही कर्मों पर नियंत्रण के भाव से है, जिससे वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है।
अनत्त / अनात्म
भगवान की प्रमुख शिक्षाओं में से एक “अनात्म” है—अर्थात पाँच स्कंधों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) को आत्मा न मानना, क्योंकि वे नश्वर, अविश्वसनीय और निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं।
अनात्म के दो अर्थ प्रचलित हैं—
- “यह आत्मा नहीं है”—पाँच स्कंधों को ‘मैं’ या ‘मेरा’ न समझो; उनसे आसक्ति न रखो।
- “आत्मा नहीं होती”—एक कठोर निषेधात्मक व्याख्या, जिसके अनुसार आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता का होना ही भ्रम है।
प्रारंभिक सूत्रों में अनात्म का उपयोग मुख्यतः एक रणनीति के रूप में आता है। ऐसा साधन जो साधक की पकड़ ढीली कर देता है, ताकि वह स्कंधों से चिपके बिना मुक्ति की दिशा में बढ़ सके।
इस विषय की गहरी समझ के लिए हमारी मार्गदर्शिका का यह लेख अवश्य पढ़ें 👉 क्या आत्मा है, या नहीं?
अतम्मयता / अ-तन्मयता
तन्मयता का सामान्य अर्थ है—किसी अवस्था में डूब जाना, उसी में अपनी पहचान खो देना, और उसी से बन जाना। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, या कोई अभिनेता अपने पात्र में इस कदर उतर जाता है कि वह उससे अलग नहीं रह पाता।
इसके विपरीत, अतम्मयता (अ-तन्मयता) का अर्थ है—उस अवस्था में डूबना नहीं, उसमें अपनी पहचान न गढ़ना, और उससे गढ़ा न जाना। जैसे कोई व्यक्ति पूरे होश में काम करता है—काम में रहता है, पर उसमें खोता नहीं; या जैसे कोई तैराक सिर पानी के ऊपर रखकर तैरता है।
स्मृतिप्रस्थान की साधना करते हुए यह अवस्था तब आती है, जहाँ भगवान कहते हैं—
उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।
धम्म में इसका अर्थ यह है कि स्मृति, समाधि, तटस्थता या किसी भी स्वभाव अथवा अनुभव में डूब न जाया जाए। किसी भी साधना या प्राप्त अवस्था से अपने-आप को सीमित और परिभाषित न किया जाए। यह न मान लिया जाए कि “यही मैं हूँ”, “यही मेरी साधना है”, या “यहीं तक पथ है।”
याद रखें कि अतम्मयता किसी आदेश—“कुछ भी न गढ़ो”—से नहीं आती, और न ही इसका अर्थ यह है कि स्मृति या समाधि जैसे आवश्यक अनुभवों को तुरंत छोड़ दिया जाए। समस्या अनुभव के होने में नहीं, बल्कि उसमें होश खोकर डूब जाने और आगे का कदम भूल जाने में है। शांति, सुख या तटस्थता स्वयं में बाधक नहीं हैं; बाधक है उनमें ही टिके रहना, उनसे ही अपने-आप को गढ़ लेना, और उन्हें ही अंतिम मान लेना।
अतम्मयता तब स्वाभाविक रूप से घटती है, जब यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हर अवस्था—चाहे कितनी ही सूक्ष्म और सुखद क्यों न हो—रचित और अनित्य है। तब चित्त अनुभव में होता है, पर उसमें डूबता नहीं।
इदप्पच्चयता / कार्य-कारण सिद्धांत
इदप्पच्चयता कार्य-कारण का वह सार्वभौमिक सिद्धांत है जिस पर बुद्ध की पूरी शिक्षा आधारित है। इसका शाब्दिक अर्थ है—“इसकी प्रत्ययता” या “इसके होने से यह होता है।”
यह सिद्धांत बताता है कि इस संसार में कोई भी घटना स्वतंत्र या अकस्मात नहीं है, और न ही यह किसी ईश्वरीय सत्ता द्वारा पूर्व-निर्धारित है। सब कुछ कारणों और परिस्थितियों के एक जाल पर निर्भर करता है। इसका मूल सूत्र है—
- “जब यह है, तब वह है।
- इसके उत्पन्न होने से वह उत्पन्न होता है।
- जब यह नहीं है, तब वह भी नहीं है।
- इसके रुकने से वह भी रुक जाता है।”
इदप्पच्चयता वह ‘नियम’ है जो बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि पटिच्चसमुप्पाद (प्रतीत्यसमुत्पाद) इस नियम का ‘दुक्ख’ के संदर्भ में विशेष अनुप्रयोग है।
इस गहरे नियम को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक लेख पढ़ें 👉 कार्य-कारण क्या है?
पटिच्चसमुप्पाद / प्रतीत्यसमुत्पाद
पटिच्चसमुप्पाद का अर्थ है—“प्रतीत्य” (आश्रित होकर) + “समुत्पाद” (साथ में उत्पन्न होना)। यह इदप्पच्चयता के सिद्धांत का वह विशेष ढांचा है जो बताता है कि जीवन में ‘दुक्ख’ की रचना कैसे होती है और उसका अंत कैसे संभव है।
इसे अक्सर १२ कड़ियों (निदानों) की श्रृंखला के रूप में समझा जाता है (अविद्या से लेकर जरा-मरण तक), लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं—
- समुदय (उत्पत्ति): यह देखना कि कैसे अविद्या और तृष्णा के कारण भव और जन्म का चक्र चलता रहता है।
- निरोध (समाप्ति): यह समझना कि जब अविद्या का पूर्णतः क्षय होता है, तो यह पूरा चक्र बिखर जाता है और दुक्ख का निरोध होता है।
यह केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अभी और इसी क्षण हमारे अनुभव में ‘मैं’ और ‘मेरे’ का भाव कैसे निर्मित हो रहा है।
इस प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या के लिए हमारी मार्गदर्शिका देखें 👉 प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है?
कम्म / कर्म
सामान्य भाषा में लोग ‘भाग्य’ या ‘किस्मत’ को कर्म कह देते हैं, लेकिन धम्म में कम्म का अर्थ नितांत भिन्न है। बुद्ध कहते हैं—“चेतनाहं, भिक्खवे, कम्मं वदामि” (भिक्षुओं, मैं चेतना/इरादे को ही कर्म कहता हूँ)।
कम्म को समझने के लिए दो बातों में भेद करना आवश्यक है—
- कम्म (कर्म): वह मानसिक चेतना या इरादा (मंशा) जिसके साथ हम कोई शारीरिक, वाचिक या मानसिक कार्य करते हैं। यह ‘बीज’ है।
- विपाक (फल): उस कम्म का परिणाम। यह वह अनुभव है जो हमें प्राप्त होता है।
हर अनुभव कम्म नहीं होता; कुछ अनुभव पुराने कम्मों का ‘विपाक’ (फल) होते हैं, और कुछ केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं (ऋतु, बीज, आदि) के कारण होते हैं। कम्म का सिद्धांत हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम ‘विपाक’ को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में हम कैसी ‘चेतना’ उत्पन्न कर रहे हैं, वह हमारे हाथ में है।
कर्म और उसके फल के गहन संबंध को समझने के लिए यह लेख पढ़ें 👉 कर्म क्या है?
पपञ्च / प्रपंच
प्रपंच—अर्थात मन की एक आदत, जिसमें कोई लगातार सोचता जाता है, तरह-तरह की बातें जोड़ता है, कल्पनाएँ करता है, पुराने अनुभवों को दोहराता है, और अपनी ही बातें मन में चलाता रहता है। यह सब सोच असली सच्चाई को छुपा देती है। यह सिर्फ “सोचना” नहीं है, बल्कि सोचने की ऐसी लत है जो मन को भटकाती है, जिससे हम सीधे अनुभव को नहीं देख पाते।
उदाहरण से समझें—मान लीजिए कोई आपको कुछ उल्टा-सीधा कह दे, जो आपको अच्छा न लगे। तो आप पहले सोचते हैं, “उसने ऐसा क्यों कहा?” फिर, “वो हमेशा ऐसा करता है।” फिर, “उसको मुझसे ही दिक्कत क्यों होती है?” फिर, “मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए…” इत्यादि इत्यादि।
यह जो बिना रुके चलने वाला सोच का सिलसिला है—यही प्रपञ्च है। यह सब असल में उस एक क्षण की सच्चाई को ढक देता है कि किसी ने बस कुछ कहा था। बस! बाकी सब आपके मन की बनाई कहानी है।
पालि सूत्रों में इसका आशय केवल विचारों की अधिकता नहीं, बल्कि ऐसे विचारों की प्रवृत्ति से है जो “स्व” की धारणाओं से उत्पन्न होकर संसार के साथ टकराव और क्लेश उत्पन्न करते हैं।
सुत्तनिपात ४:१४ में कहा गया है कि पपञ्च का मूल है—“मैं सोचने वाला हूँ” यह धारणात्मक दृष्टिकोण। जब चित्त स्वयं को “कर्ता”, “भोक्ता”, या “स्वामी” के रूप में देखता है, तब उससे जुड़ी अनेक द्वैतात्मक श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं—जैसे: “मैं/कोई पराया”, “मेरा/पराए का”, “अस्तित्व/अनस्तित्व”, “जुटाने वाला/खाने वाला”। यह दृष्टिकोण न केवल स्वयं की एक ठोस पहचान गढ़ता है, बल्कि अन्यों को भी भोग “वस्तुओं” की तरह देखता है—और यहीं से संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और दुःख का जन्म होता है।
इसलिए प्रपंच केवल मानसिक उलझन नहीं, बल्कि “वस्तुकरण” की प्रवृत्ति है—जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, संबंधों, और स्वयं को भी ऐसी ठोस श्रेणियों में बाँधता है जो अंततः क्लेशकारी सिद्ध होती हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने इसे मिटाने योग्य जड़ कहा, और उस चित्त को मुक्त बताया—जिसमें पपञ्च-सङ्ख (वस्तुकरण के विकारी विचार) शेष नहीं रहते।
नाम-रूप
नाम–रूप को हम अपने संपूर्ण अनुभव के रूप में समझ सकते हैं। सरल शब्दों में, रूप अनुभव का भौतिक पक्ष है, और “नाम” उसका मानसिक पक्ष। जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, या शरीर के रूप में उपस्थित है—वह रूप है। और जो उसे महसूस करता है, अर्थ देता है और प्रतिक्रिया की दिशा तय करता है—वह नाम है।
रूप में हमारा भौतिक शरीर शामिल है, जिसे “चार महाभूतों”—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु धातु—के रूप में समझा जाता है। यही वह आधार है जिस पर अनुभव घटित होता है: इंद्रियाँ, उनका कार्यक्षेत्र, और वह भौतिक ढाँचा जिसके बिना कोई अनुभूति संभव ही नहीं।
नाम के अंतर्गत वेदना (=अनुभूति), संज्ञा (=नजरिया), इरादा (“चेतना”), संपर्क (“फस्स”), और मनोयोग (“मनसिकार”) आते हैं। यानी जो छूआ जाता है, महसूस होता है, पहचाना जाता है, जिस पर ध्यान जाता है, और इरादे के अनुसार मन दिशा लेता है—वह सब नाम है।
इस दृष्टि से नाम–रूप कोई स्थिर या जमी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि पल–पल घटती हुई एक प्रक्रिया है। जैसे-जैसे भौतिक आयाम और मानसिक आयाम के बीच संपर्क होता है, वैसे-वैसे दोनों सक्रिय होने लगते हैं और साथ मिलकर अनुभव को आकार देते हैं। यही सतत प्रक्रिया संसार को हमारे लिए वास्तविक बनाती है।
नाम–रूप और विज्ञान एक-दूसरे पर आश्रित हैं: बिना नाम–रूप के विज्ञान टिक नहीं सकता, और बिना विज्ञान के नाम–रूप सक्रिय नहीं होता। इसी आपसी निर्भरता से जीवन का पूरा अनुभव बनता है। और इसी कड़ी को तोड़ने पर मुक्ति भी घटित होती है।
खन्ध / स्कन्ध / समूह
खन्ध का मतलब है “समूह”, “संग्रह”, या “ढेर”। यह पाँच तरह के मानसिक और शारीरिक अनुभवों का समूह है, जिनके आधार पर हम “मैं” या “मेरा” का बोध करते हैं। ये अनुभव ही हमारे जीवन की पूरी प्रक्रिया बनाते हैं। पाँच स्कन्ध होते हैं:
(१) रूप
रूप का सरल अर्थ है “भौतिक” शरीर। यह भौतिक रूप “चार महाभूत” (=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु धातु) से बनता है।
भगवान ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, “रुप्पती’ति रूपं!” अर्थात, “पीड़ित” होता है, इसलिए उसे “रूप” कहते है। किससे पीड़ित होता है? ठंड से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, मक्खी, मच्छर, पवन, धूप, रेंगनेवाले जीवों के स्पर्शों से पीड़ित होता है।
और, दुनिया के जितने भी रूप हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप के—वे सब मिलकर “रूपखन्ध” (=रूप समूह) कहलाते हैं।
इस विशाल रूप-समूह में से जिसे जिनके प्रति छन्द या राग हो, वे उसके “रूप उपादानखन्ध” (कुछ रूपों के प्रति आसक्ति) हैं।
(२) वेदना / अनुभूति
वेदना का अर्थ है—किसी अनुभव का ‘अहसास’, या कोई अनुभूति जिस स्वाद में ‘महसूस’ हो।
कई साधक सोचते हैं कि वेदना शरीर में होने वाली संवेदनाएं हैं, जैसे—झनझनाहट, खुजली या दर्द। लेकिन यह समझ बुद्ध की परिभाषा से थोड़ी भिन्न है। इसी तरह, आम बोलचाल में भी वेदना को केवल ‘पीड़ा’ या गहरे ‘इमोशन’ (भावुकता) से जोड़ दिया जाता है।
बुद्ध के अनुसार, जैसे ही हमारी इंद्रियों का किसी विषय (जैसे कोई दृश्य या शब्द) से संपर्क हो, तो मन तुरंत उसका एक ‘स्वाद’ लेता है। यह शुरुआती स्वाद या अहसास तीन प्रकार का हो सकता है—‘सुखद’, ‘दुखद’, या फिर ‘न-सुखद-न-दुखद’। इसी बुनियादी अनुभूति को बुद्ध ने ‘वेदना’ कहा है।
वेदना केवल शारीरिक ही नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है—सोमनस्स (=सौमनस्य) : मन में उठने वाला सुखद भाव, हर्ष या प्रसन्नता; और दोमनस्स (दौमनस्य) : मन में उठने वाला दुखद भाव, खिन्नता, या व्यथा।
जो शारीरिक या मानसिक अनुभूति सुखद और अच्छी लगती है, उसे सुख कहा जाता है। जो पीड़ादायक और अप्रिय लगती है, वह दुख कहलाती है। और जो न अच्छी लगती है, न बुरी—वह न सुख न दुख की अनुभूति है।
इस संदर्भ में बुद्ध का निरीक्षण है—“सुख बना रहे तो सुखद लगता है, किंतु बदलने पर दुखद हो जाता है। दुख बना रहे तो दुखद है, किंतु बदलने पर सुखद प्रतीत होता है। न सुख न दुख की अनुभूति यदि ज्ञान से जुड़ी हो (अर्थात, पहचानी जाए), तो वह सुखद है; और यदि ज्ञान से न जुड़ी हो (अर्थात, अनदेखी रह जाए), तो वही दुखद बन जाती है।”
दुनिया के जितने भी अनुभूतियाँ हो—भूत, भविष्य या वर्तमान की, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप की—वे सब मिलकर “वेदनाखन्ध” (=वेदना समूह) कहलाते हैं। इस विशाल वेदना समूह में से जिसे जिनके प्रति छन्द या राग हो, वे उसके “वेदना उपादानखन्ध” (कुछ अनुभूतियों के प्रति आसक्ति) हैं।
(३) सञ्ञा / संज्ञा / नजरिया
इसका सरल अर्थ है “पहचानना”, मानसिक लेबल लगाना, या किसी खास “नजरिए” से देखना। जैसे कोई फल देखकर उसे “सेब” कहना, या किसी आवाज़ को “घंटी” समझना। यह चीज़ों की पहचान करने वाला भाग है।
भगवान ने कहा, “सञ्जानाती’ति सञ्ञा!” अर्थात, (जिस तरह जानते या) “पहचानते” हैं, उसे “संज्ञा” कहते हैं। क्या पहचानते हैं? नीला पहचानते हैं, पीला पहचानते हैं, लाल पहचानते हैं, सफ़ेद पहचानते हैं।
संज्ञा फस्स या इंद्रिय संपर्क के कारण प्रादुर्भूत होते हैं। किंतु अभ्यास के माध्यम से हम अपने भीतर कुशल संज्ञाओं को विकसित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन रूपों के प्रति पहले हमारे गलत या अकुशल नज़रिए के कारण आकर्षण उत्पन्न होता था, उनके प्रति हम अशुभ संज्ञा विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार, जिन रूपों के प्रति पहले घृणा या द्वेष था, उनके प्रति यदि हम सद्भावपूर्ण नज़रिया अपनाएँ, तो अनेक मानसिक परेशानियों से बचा जा सकता है।
उसी तरह, सभी आसक्तियों को अनित्य, दुःख, या अनात्म जैसी संज्ञाओं के माध्यम से देखने से मुक्तिपथ में प्रगति होती है।
दुनिया के जितने भी संज्ञा या नजरिए हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप के—वे सब मिलकर “सञ्ञाखन्ध” (=नजरियों का समूह) कहलाते हैं।
इस विशाल नजरिया-समूह में से जिसे जिनके प्रति छन्द या राग हो, वे उसके “सञ्ञा उपादानखन्ध” (कुछ नजरियों के प्रति आसक्ति) हैं।
(४) सङ्खार / संस्कार
भगवान कहते हैं, “सङखतमभिसङखरोन्ती’ति सङखारा!” अर्थात, संस्कृत/रचने योग्य (वस्तुओँ) को रचते हैं, उसे “संस्कार” कहते है।
क्या रचते है? रूपत्व (=भौतिकता) के लिए रूप रचते हैं। वेदत्व (=महसूस करने) के लिए “वेदना” रचते है। संज्ञत्व (=पहचानने) के लिए “संज्ञा” रचते है। संस्कृत्व (=रचने) के लिए “संस्कार” रचते है। और, विज्ञत्व (=जानने) के लिए “विज्ञान” रचते है।
जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को गढ़कर घड़ा बनाता है या कोई लेखक सोच-समझकर कथा और पात्रों की रचना करता है, उसी तरह संस्कार वह प्रक्रिया है, जिसमें किसी वस्तु, विचार या भावना को पहले से मौजूद तत्वों को जोड़-घटाकर नया रूप दिया जाता है। यह स्वाभाविक नहीं, बल्कि गढ़ी हुई, बनाई गई या बदली हुई चीज़ होती है।
संस्कार या रचना दो रूपों में होते हैं—एक प्रक्रिया के रूप में (रचना, जो लगातार चल रही होती है) और एक परिणाम के रूप में (रचना जो अब बन चुकी है)। संस्कार के तीन प्रकार हैं:
- काय संङ्खार (शारीरिक संस्कार) – वे क्रियाएँ जो शरीर से की जाती हैं, जैसे चलना, बैठना, कूदना। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो, सांस लेना भी एक काय संस्कार है, क्योंकि यह शरीर की बनावट और अवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए आश्वास-प्रश्वास (सांस लेना और छोड़ना) को काय संस्कार कहा जाता है।
- वाची संङ्खार (वाणी संस्कार) – वे क्रियाएँ जो वाणी के माध्यम से होती हैं, जैसे बोलना, गाना, पाठ करना या चिल्लाना। हमारी वाणी तभी प्रकट होती है जब मन किसी विषय पर विचार करता है। बिना विचार किए शब्दों की संस्कार नहीं हो सकती। इसलिए वितर्क और विचार (=चिंतन करना) को वाची संस्कार कहा जाता है।
- चित्त संङ्खार (मानसिक संस्कार) – वे क्रियाएँ जो हमारे चित्त को आकार देती हैं, जैसे किसी विशेष दृष्टिकोण से कोई अनुभव करना, चित्त को संकुचित या विस्तृत करना। आध्यात्मिक दृष्टि से चित्त की संस्कार किसी खास संज्ञा (=नजरिए) से चीजों को देखकर और अनुभूति करके (“वेदना”) होती है। इसलिए संज्ञा और वेदना को चित्त संस्कार कहा जाता है।
फस्स या इंद्रिय संपर्क के कारण संस्कार संग्रह प्रादुर्भूत होता है।
साधारण व्यक्ति के लिए काया, वाणी और चित्त की संस्कार पृष्ठभूमि में लगातार चलती रहती हैं। ये तभी रुकने लगती हैं जब वह सचेत होकर उन्हें रोकने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने मन के विचारों को रोकना चाहे, तो द्वितीय ध्यान में विचार पूरी तरह थम जाते हैं। चतुर्थ ध्यान में सांस का आवागमन रुक जाता है, जिससे काया की संस्कार ठहर जाती है। और निरोध अवस्था में सभी संज्ञाएँ और वेदनाएँ निरुद्ध हो जाती हैं, तभी चित्त की संस्कार भी रुकती है।
दुनिया के जितने भी संस्कार हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप के—वे सब मिलकर “सङ्खारखन्ध” (=संस्कारों का समूह) कहलाते हैं। फस्स या इंद्रिय संपर्क के कारण संस्कार संग्रह प्रादुर्भूत होता है।
इस विशाल संस्कार-समूह में से जिसे जिनके प्रति छन्द या राग हो, वे उसके “सङ्खार उपादानखन्ध” (कुछ संस्कारों के प्रति आसक्ति) हैं।
(५) विञ्ञाण / विज्ञान
विज्ञान, चैतन्य या चेतना, यानी किसी इन्द्रिय के माध्यम से अनुभव का जानना। जैसे आँख के द्वारा रूप को जानना, कान से ध्वनि को जानना, आदि। यह केवल इंद्रियों से “जानने” की प्रक्रिया है, न कि जानने वाला “स्व”।
भगवान कहते हैं, “विजानाती’ति विञ्ञाण!” अर्थात, जो जानता है, उसे “विज्ञान” कहते हैं। क्या जानता है? क्या खट्टा है, क्या कड़वा है, क्या तीख़ा है, क्या मीठा है, क्या खारा है, क्या खारा नहीं है, क्या नमकीन है, क्या नमकीन नहीं है।
दुनिया के जितने भी विज्ञान हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप के—वे सब मिलकर “विञ्ञाणखन्ध” (=विज्ञान समूह) कहलाते हैं। नाम-रूप के कारण विज्ञान संग्रह प्रादुर्भूत होता है।
इस विशाल संस्कार-समूह में से जिसे जिनके प्रति छन्द या राग हो, वे उसके “विञ्ञाण उपादानखन्ध” (किसी विज्ञान के प्रति आसक्ति) हैं।
पञ्ञा / प्रज्ञा / अंतर्ज्ञान
प्रज्ञा वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे अनुभव को जैसा वह वास्तव में है, वैसा प्रत्यक्ष देख पाता है। यह सामान्य ज्ञान, दर्शन या बौद्धिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि यथाभूत दर्शन है। इसी अर्थ में प्रज्ञा को अपना स्वयं का अंतर्ज्ञान कहा जा सकता है—वह सीधा बोध, जो शान्त, स्पष्ट और अनासक्त चित्त से भीतर ही भीतर घटित होता है।
प्रज्ञा ध्यान से अलग नहीं, बल्कि उसी से जन्म लेती है। समथ से चित्त शांत, स्थिर और अविचल होता है; वही स्थिर चित्त जब अनुभव को “बिना पकड़े, बिना टाले” देखता है, तो वही देखना विपस्सना कहलाता है। विपस्सना कोई अलग तकनीक नहीं, बल्कि ध्यान में स्थित चित्त की देखने की क्षमता है। इस देखने में ‘विचार’ गौण हो जाते हैं और ‘स्पष्टता’ प्रधान—यहीं से प्रज्ञा का उदय होता है। इसलिए प्रज्ञा केवल विश्लेषण का परिणाम नहीं, बल्कि मौन, सजग और अविचल अवलोकन का फल है।
बुद्ध के अनुसार मुक्ति का निर्णायक तत्व प्रज्ञा है, जबकि ध्यान उसका आवश्यक आधार। ध्यान चित्त को तैयार करता है; प्रज्ञा उस तैयार चित्त से यथार्थ को भेदती है। प्रज्ञा का अर्थ है कारण–परिणाम को प्रत्यक्ष देख पाना—यह समझना कि कौन-सा कर्म दुःख की ओर ले जाता है और कौन-सा दुःख की निवृत्ति की ओर। इस अर्थ में प्रज्ञा कोई स्थिर “ज्ञान” नहीं, बल्कि एक कार्यशील कौशल है, जो अभ्यास से परिपक्व होता है। ध्यान से समर्थित यही प्रज्ञा अविद्या को क्षीण करती है, तृष्णा को काटती है और अंततः मुक्ति का द्वार खोलती है।
झान / ध्यान-अवस्था / समाधि
झान गहन ध्यान की चार अवस्थाएँ हैं, जहाँ चित्त धीरे-धीरे भटकाव या चंचलता से मुक्त होकर किसी कुशल विषय पर पूरी तरह डूब जाता है।
वहाँ न कोई दबाव होता है, न कल्पना। बल्कि शांत, एकाग्र और स्थिरता होती है। हो सकता है कि किसी को झान कोई अजीब या रहस्यमय अनुभूति लगे। किन्तु वह प्रज्ञा, शील और निरंतर अभ्यास से परिष्कृत हुई चित्त की स्वाभाविक अवस्था है।
किसी अकुशल आधार पर भी ध्यान हो सकता है, पर उसका अच्छा फल नहीं आता। लेकिन जब यही ध्यान प्रज्ञा से जुड़ा हो और आर्य मार्ग के अनुरूप हो, तब उससे आर्य फल का साक्षात्कार हो सकता है। उसे आर्य सम्यक-समाधि कहते हैं, अर्थात, जब ध्यान सात आर्य-अंगों—सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक स्मृति तक—से युक्त हो।
जब चित्त में चंचलता या भटकाव क्षीण होने लगता है और वह एक कुशल विषय पर अविचल टिक जाता है, तब साधक काम-वितर्क से ऊपर उठकर झान में प्रवेश करता है। प्रारंभिक झानों में वितर्क-विचार, प्रीति और सुख होते हैं, जबकि आगे चलकर ये भी शांत होते जाते हैं और केवल तटस्थता और निर्मल सजगता शेष रहती है।
चार रूप-झान और उनसे आगे के अरूप-आयाम , चित्त की इसी क्रमिक परिशुद्धि को दर्शाते हैं।
बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि झान स्वयं में मुक्ति नहीं हैं। वे ऊँची और सुखद अवस्थाएँ हैं, किंतु यदि उनमें आसक्ति हो जाए तो वे केवल ऊँचे ब्रह्मलोक की ओर ले जाती हैं। इसलिए झान का वास्तविक मूल्य यह है कि वे समथ के माध्यम से चित्त को इतना स्थिर और निर्मल बनाते हैं कि उसी आधार पर विपस्सना द्वारा अनित्यता, दुःख और अनात्म का यथाभूत दर्शन संभव हो सके। इसलिए झान साध्य नहीं, साधन हैं, जो चित्त को इतना स्पष्ट और अविचल बना देता है कि वह यथाभूत सत्य का साक्षात्कार कर सके।
चार झान या ध्यान-अवस्थाएँ इस प्रकार हैं:
- कोई साधक कामुकता से निर्लिप्त, अकुशल स्वभाव से निर्लिप्त—वितर्क और विचार सहित, निर्लिप्तता से जन्मे प्रीति और सुख वाले प्रथम-झान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है।
- आगे, वह वितर्क और विचार थमने पर भीतर आश्वस्त हुआ मानस एकरस होकर बिना-वितर्क बिना-विचार, समाधि से जन्मे प्रीति और सुख वाले द्वितीय-झान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है।
- आगे, वह प्रीति से विरक्ति ले, स्मृति और सचेतता के साथ उपेक्षा धारण कर शरीर से सुख महसूस करता है। जिसे आर्यजन ‘उपेक्षक, स्मृतिमान, सुखविहारी’ कहते हैं—वह उस तृतीय-झान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है।
- आगे, वह सुख और दुःख के परित्याग से, तथा पूर्व के सौमनस्य और दौमनस्य के विलुप्त होने से—न सुख, न दुःख; उपेक्षा और स्मृति की परिशुद्धता के साथ चतुर्थ-झान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है।
अरूप / अरूप-आयाम / निराकार अवस्थाएँ
अरूप का शाब्दिक अर्थ है— रूप से रहित। ये अस्तित्व के वे आयाम हैं जहाँ पदार्थ या भौतिक शरीर का पूर्ण अभाव होता है। यहाँ न कोई आकार है, न दिशा, और न ही स्थान की भौतिक सीमाएँ; यहाँ केवल सूक्ष्म मानसिक अस्तित्व शेष रहता है। इस अवस्था में सत्व ‘दिखता’ नहीं, बल्कि केवल चेतना के स्तर पर विद्यमान रहता है।
बुद्ध शिक्षा में अरूप के चार प्रमुख आयाम (“आयतन”) बताए गए हैं:
- आकासानञ्चायतन (अनंत आकाश आयाम): जहाँ रूप का बोध पूरी तरह मिट जाता है और केवल असीम, अंतहीन आकाश का अनुभव शेष रहता है।
- विञ्ञाणञ्चायतन (अनंत विज्ञान आयाम): जहाँ साधक आकाश से भी परे हटकर केवल अनंत चेतना पर एकाग्र होता है।
- आकिञ्चञ्ञायतन (आकिंचन्य/शून्य/सूना आयाम): जहाँ “कुछ भी नहीं है” (नास्ति किञ्चि) का अत्यंत सूक्ष्म और शांत अनुभव होता है।
- नेवसञ्ञानासञ्ञायतन (नैवसंज्ञा-नासंज्ञा आयाम): यह सूक्ष्मतम अवस्था है। यहाँ सञ्ञा इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि न तो उसे ‘संज्ञा’ कहा जा सकता है और न ही ‘संज्ञा से रहित’।
ये अवस्थाएँ गहरे अरूप-ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होती हैं, जहाँ साधक स्थूल शरीर और इंद्रियों की सीमाओं को लांघ जाता है। यहाँ प्रायः यह एक भ्रांति रहती है कि इन अवस्थाओं तक पहुँचने के लिए पहले चार झान (‘रूप-ध्यानों’) के क्रम से गुजरना अनिवार्य है। किन्तु ऐसा नहीं है; इन आयतनों में सीधे भी प्रवेश किया जा सकता है।
जिसे अन्य आध्यात्मिक दर्शन या धार्मिक परंपराएं ‘मोक्ष’, ‘कैवल्य’ या ‘ब्रह्म-लीन’ होना कहती हैं—जहाँ आत्मा के परमात्मा में विलीन होने या परम शून्य में समा जाने की बात की जाती है—बौद्ध दृष्टिकोण से वे अक्सर इन्हीं ‘अरूप आयामों’ की बात कर रहे होते हैं।
उन ऋषियों और साधकों ने चित्त की इस अत्यंत एकाग्र, शांत और सुखद अवस्था को ही ‘अंतिम सत्य’ मान लिया, क्योंकि वहाँ उन्हें दुःख का कोई स्थूल रूप दिखाई नहीं दिया। लेकिन बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा से देखा कि यह भव निरोध (मुक्ति) नहीं है, बल्कि एक अत्यंत लंबी अवधि वाला ‘अरूप पुनर्जन्म’ है। यह एक “सोने के पिंजरे” जैसा है—जहाँ शांति तो है, लेकिन संपूर्ण मुक्ति नहीं।
बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएँ भी अनित्य हैं और संसार के भव-चक्र के भीतर ही आती हैं। यहाँ अविद्या सुप्त अवस्था में जीवित रहती है। इसलिए, बौद्ध मार्ग में अरूप ध्यान को अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि पञ्ञा के विकास के लिए एक ऊँचा, परन्तु अस्थायी, पड़ाव माना गया है।
सेक्ख / शिक्षार्थी / साधक
सेक्ख का सरल अर्थ है—धम्म का वास्तविक विद्यार्थी। यानी ऐसा साधक जिसने केवल बुद्ध की बातों को समझा ही नहीं, बल्कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है। उसने धम्म को देखा है, मार्ग का अनुभव किया है, शायद कुछ फल भी पाया है, लेकिन अभी उसका अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। उसके भीतर अब भी अनुशासन, सावधानी और निरंतर साधना की आवश्यकता बनी रहती है।
इसलिए सेक्ख वह है जो सीख रहा है, किताबों से नहीं, बल्कि अपने आचरण, शील और ध्यान के अभ्यास से। वह जानता है कि मार्ग क्या है और उस पर चल भी रहा है, लेकिन अभी मंज़िल तक पहुँचा नहीं है। तकनीकी रूप से, श्रोतापन्न , सकृदागामी और अनागामी तक के सभी आर्य शिष्य सेक्ख कहलाते हैं।
इसके विपरीत असेक्ख वह है जिसके लिए सीखने को कुछ शेष नहीं रहता। यह अवस्था अरहंत की है, जहाँ समस्त आस्रव क्षीण हो चुके होते हैं, मार्ग पूरा हो चुका होता है और अब न अभ्यास शेष है, न साधना की कोई कमी। जहाँ सेक्ख “पथ पर चल रहा है”, वहीं असेक्ख “पथ को पूर्ण कर चुका है”।
अरहं / अरहंत
अरहं का शाब्दिक अर्थ है, “काबिल” व्यक्ति। अर्थात, जो दसों संयोजनों (=बेड़ियाँ) यही इसी लोक में तोड़ देता है, उसे वाकई काबिल या अरहंत माना जाता हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी दुःखों का अन्त हो जाता है, और वह जन्म-मरण के भटकन से आज़ाद हो जाता है।
कोई भिक्षु आस्रवों के क्षय होने से अनास्रव होकर, इसी जीवन में चेतोविमुक्ति और प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर, (अर्हत्व) प्रत्यक्ष-ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। वे अरहंत होकर आस्रव खत्म करते हैं, ब्रह्मचर्य परिपूर्ण करते हैं, कर्तव्य समाप्त करते हैं, बोझ को नीचे रखते हैं, परम-ध्येय प्राप्त करते हैं, भव-बंधन को पूर्णतः तोड़ देते हैं, सम्यक-ज्ञान से विमुक्त होते हैं, उनके लिए कोई (पुनर्जन्म के) दुष्चक्र का पता नहीं चलता।
— महापरिनिब्बान सुत्त + मज्झिमनिकाय २२: अलगद्दूपमसुत्त
अरहंत का शील-स्कन्ध और समाधि-स्कन्ध के साथ, प्रज्ञा-स्कन्ध भी परिपूर्ण हो जाता है। उसकी संपूर्ण अविद्या नष्ट होती है, और वह जाग जाता है।
वह, दस धम्मों से परिपूर्ण होता है—आर्य अष्टांगिक मार्ग के आठ अंग—सम्यक-दृष्टि… सम्यक-समाधि, और सम्यक-ज्ञान और सम्यक-विमुक्ति।
अनागामी
अर्थात, ऐसा आर्य व्यक्ति जिसने धम्म का साक्षात्कार इतनी गहराई से कर लिया हो कि उसके कामलोक के सभी बंधन टूट जाए। तब, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पुनः इस लोक में कभी नहीं लौटता। बल्कि मरने के बाद सबसे ऊँचे शुद्धवास ब्रह्मलोक में सचेत प्रकट (“ओपपातिक”) होता है, और वही अंतिम ‘अरहंत’ अवस्था प्राप्त कर परिनिवृत होता है।
“कोई आर्यश्रावक निचले पाँच संयोजन तोड़कर स्वप्रकट होगा, वही परिनिर्वाण प्राप्त करेगा, अब इस लोक में नहीं लौटेगा।”
—दीघनिकाय २८: सम्पसादनीयसुत्त
वह पहली पाँच बेड़ियाँ संयोजन —स्व-धारणा की दृष्टि, उलझन, कर्मकाण्ड और व्रत में अटकाव, कामेच्छा, और दुर्भावना—मानवलोक में तोड़ देता हैं, और अगली पाँच ब्रह्मलोक में तोड़ता है।
उसका समाधि-स्कन्ध परिपूर्ण होता है। अर्थात, वह चार ध्यान-अवस्थाओं को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सम्यक-समाधि में उसे निपुणता हासिल होती है।
किन्तु, उसे ऊपरी पाँच संयोजन बाधित करते हैं। अर्थात, उसे भौतिक-रूपता में और अरूपता में राग (=दिलचस्पी) होती है। वह अहंभाव, बेचैनी, और अविद्या से बाधित होता है।
अनागामी व्यक्तियों के पाँच प्रकार होते हैं:
“पाँच अनागामी होते हैं—
- (इस लोक और परलोक के) बीच में परिनिवृत होने वाला,
- (शुद्धवास) पहुँचने पर परिनिवृत होने वाला,
- बिना (प्रयास का) संस्कार बनाए परिनिवृत होने वाला,
- (प्रयास का) संस्कार के साथ परिनिवृत होने वाला,
- चढ़ती धारा में (सर्वोच्च लोक) ‘अकनिट्ठ’ जाने वाला।”
सकदागामी / सकृदागामी
अर्थात, जो केवल एक बार और इस लोक में जन्म लेकर अपने दुःखों का अन्त करे।
कोई आर्यश्रावक तीन संयोजन तोड़कर, राग-द्वेष-मोह को दुर्बल कर सकृदागामी बनता है, जो इस लोक में दुबारा लौटकर अपने दुःखों का अन्त करता है।
अर्थात, जो अपने अगले जन्म में निश्चित परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। वह दस में से पहली तीन बेड़ियाँ—स्व-धारणा की दृष्टि, उलझन, और कर्मकाण्ड और व्रत में अटकाव—तोड़ता है। साथ ही, कामुकता और दुर्भावना को दुर्बल बनाता है, उनको स्थूल से सूक्ष्म बनाता है। अर्थात, उसे क्रोध और कामुकता उतनी तीव्रता से नहीं जागती है, जितनी किसी साधारण मानव को जागती है।
सोतापन्न / श्रोतापन्न
श्रोतापन्न का शाब्दिक अर्थ है—“जो धम्म की श्रोत (=धारा) में प्रवेश कर चुका है”। यह श्रोत है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो व्यक्ति को परममुक्ति, अर्थात निर्वाण, तक ले जाती है। इसलिए श्रोतापन्न को अक्सर “आर्य अष्टांगिक मार्ग में स्थित” कहा जाता है।
प्रारंभिक सूत्रों में उनका ऐसा वर्णन मिलता है —
तब धम्म देख चुका, धम्म पा चुका, धम्म जान चुका, धम्म में गहरे उतर चुका (अमुक व्यक्ति) संदेह लाँघ कर परे चला गया, जिसे अब कोई प्रश्न न रहा, जिसे निडरता प्राप्त हुई, जो शास्ता के शासन (=शिक्षा) में स्वावलंबी हुआ।
श्रोतापति की ‘आस्था’ के लिए अवेच्च शब्द का प्रयोग होता है, जिसका सरल अर्थ है “अनुभवजन्य”, यानि जिसने अनुभव कर लिया हो, या जिसकी आस्था ‘सत्यापित’ हो चुकी हो। ऐसा व्यक्ति अब केवल विश्वास के मारे “मानता” नहीं मानता, बल्कि वह “जानता” है। क्योंकि उसने स्वयं देखा और अनुभव किया है। उसकी श्रद्धा अब अंधी नहीं, बल्कि “अनुभवजन्य और सत्यापित” हो चुकी है।
उसे बुद्ध में एक शास्ता या शिक्षक के रूप में अनुभवजन्य आस्था होती है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया है और वे परिणाम प्राप्त किए हैं जिनका बुद्ध ने वर्णन किया है। एक श्रोतापन्न ने चार आर्य सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव किया होता है, इसलिए उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली होती है कि यह शिक्षाएँ वास्तव में इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती हैं।
श्रोतापन्न का तकनीकी वर्णन कुछ इस प्रकार होता है —
कोई आर्यश्रावक तीन संयोजन तोड़कर श्रोतापन्न बनता है—अ-पतन स्वभाव का, निश्चित संबोधि की ओर अग्रसर।
श्रोतापतिफल दस में से तीन संयोजन (=बेड़ियाँ)—
- स्व-धारणा की दृष्टि,
- संदेह/उलझन,
- कर्मकाण्ड और व्रत में अटकाव
— तोड़ने पर मिलता हैं। यह आर्य-अवस्था प्राप्त होते ही, व्यक्ति हमेशा के लिए दुर्गति (नर्क, प्रेतलोक या पशुयोनि) से छूट जाता है।
श्रोतापन्न के प्रमुख लक्षण होते हैं। उसकी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था सत्यापित होती है। वह बहुत दानी होता है। और वह अंतर्ज्ञानी होता है। सूत्रों के अनुसार, उसका शील-स्कन्ध परिपूर्ण होता है। अर्थात, यदि वह गृहस्थ हो तो उसके पाँच शील अटूट होते हैं, भिक्षु हो तो भिक्षुओं के प्रमुख पातिमोक्ख शील अटूट होते हैं।
श्रोतापन्न तीन तरह के होते हैं—
- सत्तक्खत्तु परम—जो देव या मानवलोक में अधिक से अधिक सात बार जन्म लेकर जन्म-मरण की शृंखला तोड़ता है।
- कोलङ्गकोल—जो ऊँचे कुलीन परिवारों में दो या तीन बार जन्म लेकर अपने दुःखों का अन्त करता है।
- एक बीजी—जो केवल एक बार और मानवलोक में जन्म लेकर संसार से मुक्त हो जाता है।
धम्मानुसारी / सद्धानुसारी
धम्मानुसारी वह व्यक्ति होता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अपनी उपलब्ध, सीमित प्रज्ञा से उन्हें जाँचता-परखता है और फिर स्वीकार करता है।
इस अवस्था में उसके कुछ-कुछ आस्रव क्षीण होने लगते हैं, यद्यपि वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते। साथ ही उसमें पाँच इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इन पाँचों इंद्रियों को साधने और बढ़ाने से उसकी धर्म में क्रमशः प्रगति होती है। इसका उल्लेख मज्झिमनिकाय ७० में मिलता है।
इसके विपरीत सद्धानुसारी वह होता है, जिसमें बुद्ध या किसी भिक्षु के प्रति सीमित मात्रा में श्रद्धा और प्रेम होता हैं। वह मुख्यतः इसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के आधार पर शिक्षाओं को स्वीकार करता है। उसकी भी वही पाँच इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इन इंद्रियों के विकास के साथ उसकी भी धर्म में उन्नति होती है।
इन दोनों को ही सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अर्थात, श्रोतापत्ति-फल का साक्षात्कार करने में जुटे हुए माना जाता है। यानि वे उस मार्ग पर चल रहे होते हैं जो उन्हें श्रोतापन्न बनने की ओर ले जाता है।
उनके संबोधि के अवसर के बारे में भगवान उपमा देते हुए कहते हैं —
जिस तरह एक नन्हा बछड़ा, जो अभी-अभी पैदा हुआ हो, वह भी अपने माँ गाय के पुकारने पर गंगा के प्रवाह को काटते हुए, उसे लाँघ कर पार करता है—उसी तरह, जो भिक्षु धम्मानुसारी और श्रद्धानुसारी हैं—वे भी मार के प्रवाह को काटते हुए लाँघ कर पार करते हैं।
अर्थात, उनका ‘संबोधि की ओर अग्रसर होना’ १००% निश्चित नहीं होता, जिस तरह किसी श्रोतापन्न का होता है। बल्कि उन्हें निरंतर किसी आर्यश्रावक से प्रेरणा लेते रहने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि उनकी अक्सर सद्गति ही होती है।
संयुक्तनिकाय २५.१ और ४८:१८ के अनुसार, जैसे-जैसे उनकी पाँच इंद्रिय—श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा—परिपक्व होती हैं, वे अपने इसी जीवन में मृत्युपूर्व श्रोतापत्ति फल को प्राप्त करते हैं।
आनेञ्ज / अविचलता
अविचलता, या “आनेञ्ज” अवस्था, चित्त की एक विशिष्ट दशा है, जिसे कामुकता से परे माना गया है। इस अवस्था में चित्त की समस्त चंचलता और विचलन शांत हो जाते हैं। इसके अंतर्गत कुल तीन अवस्थाएँ सम्मिलित हैं—
- “चतुर्थ-ध्यान अवस्था”,
- “अनन्त आकाश आयाम”
- “अनन्त विज्ञान आयाम”
इन तीन अवस्थाओं में कामुकता, काम-संज्ञा, या रूप-संज्ञा पूर्णतः निरस्त होते हैं और चित्त अविचलता को प्राप्त करता है।
यद्यपि अट्ठकथा के अनुसार चारों ही अरूप आयाम अविचलता के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तथापि मज्झिमनिकाय १०५ और मज्झिमनिकाय १०६ से यह निःसंदेह स्पष्ट होता है कि “आकिञ्चञ्ञायतन” (शून्य-आयाम), “नेवसञ्ञानासञ्ञायतन” (न-संज्ञा–न-असंज्ञा आयाम), तथा “निरोध-समापत्ति” इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
इसका कारण यह है कि अविचलता का आधार केवल “संज्ञा” होती है, और यह संज्ञा शून्य-आयाम में, अथवा उससे परे, अपना अस्तित्व खो देती है।
सम / विषम
जब कोई मार्ग ऊबड़-खाबड़ और कठिन होता है, तो यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ता है। जब संगीत बेसुरा और बेताल होता है, तो सुनने वालों को बेचैनी होती है। जब कोई गाड़ी असंतुलित होकर झटके खाती है, तो सवार को परेशानी होती है। इसी तरह, जब कोई व्यक्ति विषम आचरण करता है—असंगत विचार, असंयमित वाणी और अनियमित जीवनशैली अपनाता है—तो वह न केवल स्वयं दुखी रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है। मरणोपरांत वह विषम लोक में गिरता है।
इसके विपरीत, सम होना सहजता, सुगमता और कल्याण का प्रतीक है। जैसे एक समतल, सुंदर मार्ग पर चलना सुखद अनुभव होता है, वैसे ही समचित्त व्यक्ति के साथ रहना भी शांति देता है। जैसे सुरीला, तालबद्ध संगीत मन को आनंदित करता है, वैसे ही सम आचरण से समाज में सौहार्द और संतुलन बना रहता है। और अगले जन्मों में भी, सम जीवन जीने वाला सम लोक में जाता है।
समण / श्रमण
श्रमण का व्यावहारिक अर्थ है भिक्षु या संन्यासी। ऐसे लोग जिन्होंने ब्राह्मणी नीतियों, चतुर्वर्ण की सामाजिक-संस्कार, और सांस्कृतिक पहचान को त्याग दिया है, और जो किसी भिन्न मार्ग पर चल रहे हैं। चूँकि ‘समण’ शब्द 'सम' से बनता है, यह स्पष्ट है कि वे लोग ब्राह्मणी मार्ग को 'विषम' मानते होंगे।
“श्रमण्यता” का अर्थ है जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाना। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को बताया कि झूठ बोलने से जीवन की श्रमण्यता नष्ट होती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का आंतरिक संतुलन और समता बिगड़ने के साथ-साथ बाहरी समंजस्य और स्पष्टता भी खत्म हो जाती है।
उदाहरण के लिए, एक साज़िंदे को लें; जब वह अपने वाद्य यंत्र को सही सुर में लाने के लिए ट्यून करता है, तो वह वाद्य के आंतरिक संतुलन के साथ बाहरी श्रोताओं के साथ भी मधुर संतुलन बनाता है। इसी तरह, श्रमण अपने कर्मों को सृष्टि के नियमों के अनुसार ढालता है, जिससे उसकी भीतरी और बाहरी जीवनधारा में शांति, स्थिरता, मधुरता, संतुलन और समंजस्यता स्थापित होती है। इस प्रकार, श्रमण का जीवन केवल उसके व्यक्तिगत विकास को ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है।
भगवान बुद्ध के समय में भारत में कई प्रमुख श्रमण परंपराएँ विद्यमान थीं, जो ब्राह्मण धम्म और वेदों से अलग एक स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थीं। इन परंपराओं का मुख्य उद्देश्य आत्ममुक्ति की खोज करना था, और ये पारंपरिक ब्राह्मणवादी कर्मकांडों या वेदों पर आधारित धम्म के प्रति संदेह रखते थे। श्रमणों ने सत्य की खोज में संन्यास, तपस्या, और व्यक्तिगत अनुभव को प्रमुख मानते हुए धम्म को धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि में देखा।
श्रमण परंपराएँ बौद्धिक और दार्शनिक रूप से अत्यंत प्रगतिशील थीं, जिन्होंने निष्पक्षता और तर्क पर आधारित नए सिद्धांत विकसित किए। इन परंपराओं ने वेदों की संप्रभुता और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, यज्ञ और हवन जैसे कर्मकांडों के बजाय आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनका यह साहसिक दृष्टिकोण तत्कालीन भारत के धार्मिक और बौद्धिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित कर रहा था, जहाँ वे व्यक्तिगत सत्य को सर्वोच्च मानते थे। इस प्रकार, श्रमण परंपराओं ने भारत के समाज और दर्शन में एक गहरा बदलाव लाने की शुरुआत की, जो बुद्ध के समय में और भी सशक्त रूप से उभरा। यहाँ कुछ प्रमुख श्रमण परंपराओं का उल्लेख है:
१. जैन (निगंठ): जैन श्रमण परंपरा उस समय की प्रमुख परंपराओं में से एक थी। भगवान महावीर, जो जैन धम्म के २४वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इस परंपरा के संस्थापक थे। जैन धम्म अहिंसा और कठोर तपस्या पर बल देता था, जिसमें उपवास, आत्मपीड़ा और आत्मसंयम की कठोर साधनाएँ शामिल थीं।
२. आजीवक: आजीवक परंपरा का नेतृत्व मक्खलि गोसाल कर रहे थे। आजीवकों का विश्वास नियतिवाद (नियति) पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया था कि जीवन की हर घटना पूर्व-निर्धारित है और मनुष्य के पास अपने कर्मों का कोई नियंत्रण नहीं है।
३. लोकायत: लोकायत या चार्वाक परंपरा भोगवादी और नास्तिक थी। इस परंपरा ने पुनर्जन्म, कर्म, और आत्मा के अस्तित्व को नकारा। उनका मानना था कि भौतिक जगत ही एकमात्र वास्तविकता है और जीवन का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय-सुख की प्राप्ति है।
४. अज्ञेयवाद: अज्ञेय संप्रदाय के लोग संशयवादी या अज्ञेयवादी थे, जो किसी भी ज्ञान के दावे को अस्वीकार करते थे। संजय बेलट्ठिपुत्त इस परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि थे। वे किसी भी दार्शनिक या धार्मिक प्रश्न पर निश्चित उत्तर देने से इनकार करते थे, और कहते थे कि कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता।
५. पूरण कश्यप का संप्रदाय: पूरण कश्यप ने नैतिकता और कर्म के सिद्धांत को नकारा। उनका मानना था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई नैतिक परिणाम नहीं होता (अक्रियावाद)।
६. पकुध कच्चायन का संप्रदाय: पकुध कच्चायन ने सात शाश्वत तत्वों की धारणा प्रस्तुत की, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुःख और जीवन शामिल थे। उनका मानना था कि ये तत्व शाश्वत और अटल हैं, और इनके बीच कोई वास्तविक अंतःक्रिया नहीं होती। उन्होंने नैतिकता और आचार के महत्व को भी खारिज कर दिया।
७. बौद्ध धम्म: स्वयं बुद्ध, जिन्हें ‘महाश्रमण’ कहा जाता था, ने एक श्रमण परंपरा का नेतृत्व किया, जिसने अतितपस्या और इंद्रिय-सुख की अति के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया। बौद्ध धम्म का केंद्रबिंदु चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है।
भगवान बुद्ध के पश्चात भी अनेक श्रमण परंपराएँ चलती रहीं। इन परंपराओं ने भारतीय बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला —
१. कबीरपंथ: कबीर ने वेदों और कुरान दोनों की आलोचना की और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते हुए एक सीधा, व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग बताया। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और समता का संदेश दिया और जाति-पाति, धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता की कड़ी आलोचना की।
२. सिख धम्म: गुरु नानक ने भी ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और सामाजिक बंधनों का विरोध किया। उन्होंने एक निराकार ईश्वर के प्रति भक्ति और साधारण जीवन में सत्य, सेवा, और समानता के सिद्धांतों पर जोर दिया। सिख धम्म व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा के संयुक्त मार्ग पर आधारित है, जो श्रमण परंपराओं की स्वतंत्रता और तर्कशीलता के तत्वों से प्रभावित है।
३. सूफीवाद: सूफी संत, इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बाहरी धार्मिक नियमों से अधिक आंतरिक प्रेम, अनुभव, और भक्ति पर जोर देते हैं। सूफियों ने समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाया, और धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए ईश्वर के साथ सीधे अनुभव के महत्व को बताया। भारत में सूफी संतों, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया और मुईनुद्दीन चिश्ती, ने आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का व्यापक प्रभाव छोड़ा।
४. संत परंपरा (रैदास, तुलसीदास, मीराबाई): संत परंपरा में कई कवि-संत हुए जिन्होंने भक्ति, सामाजिक समानता, और धम्म के आडंबर से परे एक सरल और व्यक्तिगत ईश्वरभक्ति की ओर लोगों को प्रेरित किया। इनमें भी कर्मकांडों और जातिगत बंधनों का विरोध दिखता है।
५. नाथपंथ (गोरखनाथ): नाथ संप्रदाय हठयोग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। इसका श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है, जिन्होंने श्रमण परंपराओं की धारा को आगे बढ़ाया और तपस्या और ध्यान के जरिए मुक्ति की खोज को प्रमुख रूप से रखा।
६. ओशो: ओशो रजनीश एक आधुनिक गुरु और दार्शनिक थे, जिनका जीवन विवादों से घिरा रहा। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक आडंबरों को चुनौती देते हुए व्यक्तिवाद को प्राथमिकता दी और विवादास्पद ध्यान की तकनीकों के माध्यम से लोगों को अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में मदद की।
इन सभी परंपराओं में हम देखते हैं कि वे पारंपरिक धम्म के कर्मकांडों को अस्वीकार करते हुए एक नया, व्यक्तिगत और अनुभववादी आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं।
परिब्बाजक / घुमक्कड़
दुनिया भर में ऐसे घुमक्कड़ मिलते हैं, जो अपनी स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दूसरे देशों की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए यात्रा करते रहते हैं। प्राचीन जम्बूद्वीप में इन्हें “परिव्राजक” कहा जाता था, जबकि आधुनिक पश्चिमी दुनिया में इन्हें “हिप्पी” के रूप में पहचाना जाता है। इनकी जीवनशैली सामान्य सामाजिक नियमों से हटकर होती है। भारतीय परंपरा में राहुल सांकृत्यायन जैसे घुमक्कड़ विद्वान इसी प्रवृत्ति के उदाहरण थे, जो ज्ञान की खोज में यात्रा करते रहे।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ऐसे घुमक्कड़ों का मानसिक स्वभाव “प्रवाही और विद्रोही” होता है। वे पारंपरिक ढाँचों और समाज द्वारा स्थापित स्थिरता को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका हृदय स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होती है। यह विद्रोही मानसिकता उन्हें समाज के हर अनुशासन को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, कभी-कभी उनके अपने भीतर के बंधनों को भी।
वे तात्कालिक अनुभवों और क्षणिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थायित्व उनके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। उनकी विद्रोही ऊर्जा उन्हें संस्कारत्मक और अनूठा बनाती है, लेकिन यह अस्थिरता और गहरे संबंधों की कमी का कारण भी बन सकती है। ऐसे दिमाग को नियंत्रित करने और दिशा देने में केवल गहरे बोध वाले गुरु ही सफल हो सकते हैं, जैसा कि ओशो रजनीश ने अपने शिष्यों के साथ किया।
सूत्रों में सुनने मिलता है कि बुद्ध ऐसे ही घुमक्कड़ों को धम्म बताने का प्रयास करते हैं। उन घुमक्कड़ों को ठोस और निर्णायक मार्ग के बारे में सुनना रोचक और प्रेरणादायक तो लगता है, लेकिन उनके प्रवाही और विद्रोही स्वभाव के कारण, वे अक्सर इस मार्ग पर चलने से कतराते हैं या भटक जाते हैं।
समथ / निश्चलता
समथ का अर्थ है—चित्त की स्थिरता और निश्चल एकाग्रता।
यह अभ्यास मन को विक्षेप और चंचलता से मुक्त कर, एक निःशब्द और स्थिर स्थिति में लाता है—जैसे साँस या शरीर की अनुभूति पर निरंतर टिकना। जब चित्त एक ही आधार पर स्थिर होता है, तो उसमें सुख, सहजता और प्रफुल्लता उत्पन्न होती है। यही है समथ, जो चित्त को भीतर टिकने योग्य बनाता है।
समथ का अभ्यास समाधि के रूप में जाना जाता है, जिसका चरम रूप है— झान , यानी ध्यान की गहन अवस्थाएँ। बिना इस मानसिक स्थिरता के, विपस्सना गहराई नहीं पकड़ सकती। यह टिकाव चित्त को उस स्थायित्व में पहुँचाता है, जहाँ से वह अनित्य अनुभवों को स्पष्ट रूप से देख सकता है—बिना उलझे, बिना डगमगाए।
यद्यपि समथ और विपस्सना को कभी-कभी अलग पथ माना जाता है, प्रारंभिक सूत्रों में ये एक ही मार्ग के दो चरण माने गए हैं। जैसे चलने के लिए एक पैर से सहारा लेकर दूसरा आगे बढ़ता है—उसी तरह समथ चित्त को टिकाता है, और विपस्सना उस टिके हुए चित्त से यथार्थ को देखती है। एक को छोड़े बिना दूसरा संभव नहीं।
बुद्ध ने बताया कि जैसे सीढ़ी चढ़ते समय एक पायदान पर पैर टिकाकर दूसरा ऊपर रखा जाता है—वैसे ही समथ और विपस्सना एक-दूसरे को सहारा देते हुए चित्त को ऊपर उठाते हैं। समथ स्थिरता देता है, जिससे विपस्सना गहराई पाती है। फिर समथ और ऊपर उठाता है, जिससे और गहरी अंतर्दृष्टि संभव होती है।
इस तरह, समथ केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि मुक्ति का आधार है। यह चित्त को इतना परिष्कृत करता है कि वह अपने बंधनों को पहचानकर, उन्हें धीरे-धीरे छोड़ सके। इसलिए समथ कोई साधारण ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि निर्वाण की ओर बढ़ने वाली अनिवार्य नींव है।
विपस्सना / अंतर्दृष्टि
विपस्सना का अर्थ है—चीज़ों को वैसे देखना, जैसे वे वास्तव में हैं। यह देखने का ऐसा ढंग है जो बनावट, भ्रम और मान्यताओं के आवरण को हटाकर अनुभव की मूल प्रकृति को उजागर करता है।
शरीर और मन की जो भी प्रक्रियाएँ हैं—वे किसी-न-किसी संयोग, शर्त या संस्कार के आधार पर घटती हैं; और उनमें “मैं” या “मेरा” जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं होती। विपस्सना कोई चलन या केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक दृष्टि है—जो सजगता, प्रज्ञा और सूक्ष्मता से पनपती है।
जब चित्त समथ के आधार पर स्थिर हो जाता है, तभी वह इस दृष्टि को गहराई से साध पाता है। यह अभ्यास जागरूक होकर देखना सिखाता है कि संस्कार कैसे आकार में आते हैं, कैसे टिकते हैं, और कैसे समाप्त हो जाते हैं—और उन्हें अनावश्यक रूप से पकड़ने की प्रवृत्ति कैसे दुख को जन्म देती है।
इस अभ्यास का लक्ष्य केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि वैराग्य है—वह शीतल अंतर्ज्ञान जिससे चित्त आसक्ति छोड़ देता है। जब साधक अनुभवों को अनित्य, दुःख और अनात्म रूप में बार-बार देखता है, तब उनके प्रति मोह ढीला होने लगता है, भंग होने लगता है। और यही ढीलापन धीरे-धीरे मुक्ति का द्वार खोलता है—वह अवस्था, जहाँ चित्त न किसी चीज़ से बँधता है, न किसी अनुभव में उलझता है।
विपस्सना का मार्ग— इदप्पच्चयता (कारण और परिणाम) को जानने का अभ्यास है।
“जब यह होता है, तब वह होता है। जब यह नहीं होता, तब वह भी नहीं होता।”—इस सीधे साक्षात्कार के आधार पर चित्त को यह समझ आता है कि दुःख किन प्रक्रियाओं से बँधा है, और कौन-सी प्रवृत्तियाँ उसे दोहराती हैं। इस समझ से धीरे-धीरे वे संस्कार निरुद्ध होते हैं, जो दुःख को जन्म देते थे। यही है बोध, और यही है विमुक्ति की राह।
संसार
संसार का अर्थ है—संसरण या सतत भ्रमण, अर्थात् बार-बार जन्म-मरण में भटकना। यह कोई तय यात्रा नहीं, बल्कि चेतना की वासनापूर्ण गति है—जो अनादिकाल से आरम्भ होकर तृष्णा और उपादान के कारण निरंतर चलती रहती है। बुद्ध ने संसार को केवल “जीवनों की श्रृंखला” नहीं कहा, बल्कि दुःख क्षेत्र बताया, जहाँ कोई स्थायी समाधान नहीं है, कोई अंतिम ठहराव नहीं है। यह भ्रमण किसी “आत्म-खोज” के रूप में नहीं, बल्कि अज्ञान के मारे भटकना है।
संसार केवल भविष्य में पुनर्जन्म की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में भी चलता है—जब चित्त किसी विचार, भावना या पहचान में रम जाता है। इसीलिए बौद्ध परंपरा में संसार से मुक्ति का अर्थ है—भीतर की यात्रा शुरू करना, और देखना कि कैसे चित्त बार-बार ‘मैं’ और ‘मेरा’ के भ्रम में उलझ कर नया संसार रचता है। संसार से निकलने का मार्ग है—इस प्रक्रिया को देखना, समझना और उसे रोक देना। और उस विराम का नाम है: निर्वाण।
संवेग
संवेग का अर्थ है—वह भीतर की हिलावट जो जीवन की अनित्यता, संसार की असारता, और सांसारिक जीवन की व्यर्थता का साक्षात्कार करते हुए उपजती है। यह केवल दुःख नहीं, बल्कि एक जाग्रत बेचैनी है, जो मन को झकझोर कर कहती है: “यह जीवन यूँ ही नहीं गँवाना चाहिए।” यह वह क्षण होता है जब साधक को जन्म-मरण के चक्र की निरर्थकता स्पष्ट दिखने लगती है—और यहीं से धम्म की ओर उसकी यात्रा आरंभ होती है।
अनेक साधकों को संवेग जागने पर ही वे सांसारिक जीवन त्यागकर धम्ममार्ग अपनाते हैं। संवेग जब प्रज्ञा और श्रद्धा से जुड़ता है, तो केवल मानसिक व्याकुलता नहीं रह जाता—बल्कि मुक्ति की ओर ले जाने वाला शक्ति-स्रोत बन जाता है। पर यदि इस जागरण में कोई दिशा न हो, तो यह भाव निराशा या अवसाद में बदल सकता है। इसलिए संवेग के साथ आवश्यक है—पसाद।
पालि शब्द “पसाद” का अर्थ है—श्रद्धा से उत्पन्न हुई आंतरिक स्पष्टता, संतुलन और विश्वास। यह वह निर्मल भाव है जो बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति एक गहरी आस्था से उत्पन्न होता है, जो साधक को यह बोध कराता है कि मुक्ति सम्भव है। संवेग भीतर से जगाता है, और पसाद उस जगे हुए चित्त को संभालता है। इसलिए पालि सूत्रों में दोनों का उल्लेख साथ-साथ आता है—जैसे आँख में आँसू हो, और उसी में प्रकाश भी। ये दोनों भाव मिलकर साधक को जगाकर मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।
विनय
विनय का अर्थ है—“हटाना” या “दूर करना”, यानी व्यवहार से दोषों को दूर करना।
जब कोई साधक उपसंपदा लेकर भिक्षु बनता है, तो वह अपने मन को नम्रता, अनुशासन और जागरूकता के साथ प्रशिक्षित करता है। यही संघ की रीढ़ है। विनय सिर्फ बाहरी नियम नहीं, बल्कि संघ में संयम, ईमानदारी और पारस्परिक सम्मान से रहने का आधार है। इसका मकसद सज़ा देना नहीं, बल्कि आचरण को शुद्ध और मजबूत बनाना है।
विनय-पिटक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण और अनुशासन की पूरी व्यवस्था है—जिसमें नियम, संघ की कार्यप्रणालियाँ, और गलती होने पर उसके समाधान की विधियाँ शामिल हैं। यह पिटक आज छह खंडों में सुरक्षित है। इसमें भिक्षुओं के लिए २२७ नियम और भिक्षुणियों के लिए ३११ नियम बताए गए हैं।
ये नियम किसी न किसी खास घटना के उत्तर में बने—इसलिए विनय सिर्फ नियमों की सूची नहीं, बल्कि संघ के इतिहास, भिक्षु जीवन के अनुभवों और बुद्ध की व्यावहारिक समझ का जीवित साहित्य भी है।
आचरिय / उपज्झाय / अजाह्न
आचार्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है—“जो आचार (=आचरण) सिखाता है”। इसका सामान्य अर्थ है—ऐसा शिक्षक या गुरु जो धम्म, विनय या ध्यान-साधना में दूसरों का मार्गदर्शन करता है।
प्रारंभिक भिक्षुसंघ में इस भूमिका के लिए प्रचलित शब्द था उपज्झाय—जो “उपाध्याय” का पालि रूप है। उपज्झाय वह होता था जो किसी प्रव्रजित व्यक्ति को श्रावक-संघ में दीक्षा देता, उसे धम्म और विनय के अनुरूप जीवन में स्थिर करता, और आचार, अनुशासन व अभ्यास में उसका मार्गदर्शक व संरक्षक बनता।
वह न केवल प्रव्रज्या (सामणेर दीक्षा) या उपसंपदा (भिक्षु दीक्षा) प्रदान करता, बल्कि दीक्षित शिष्य के संपूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन की निगरानी और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता। यही कारण है कि उपज्झाय की भूमिका को विनय में अत्यंत गंभीर और उत्तरदायी माना गया है।
जैसे भारत में बाद के काल में “गुरु” शब्द अधिक प्रचलित हुआ, उसी प्रकार थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया आदि देशों में पालि “आचार्य” से निकला हुआ शब्द “अजाह्न” प्रचलन में आया—जो आज भी वहाँ के ध्यानगुरुओं और वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए आदरपूर्वक प्रयुक्त होता है।
इस प्रकार, चाहे वह उपज्झाय हो, आचार्य हो, या अजाह्न—इन सबका उद्देश्य एक ही है: धम्म और विनय के मार्ग पर दूसरों को स्थिर करना। असली और नकली गुरु की पहचान करने के लिए हमारा यह लेख पढ़ें 👉 गुरु की पहचान।
उपोसथ
उपोसथ का शाब्दिक अर्थ है—“निकट आना”, अर्थात “धम्म-विनय” के समीप आकर चित्त शुद्धि करना। यह विशेष साधना-दिन होता है, जो पूर्णिमा, अमावस्या, और दोनों अष्टमी तिथियों (चतुर्दशी/अष्टमी) पर आता है, अर्थात, महीने में चार।
इसकी परंपरा बुद्धपूर्व काल में भी थी, किंतु बुद्ध ने इसे धम्मानुकूल रूप देकर, गृहस्थों और भिक्षुओं, दोनों के लिए विशुद्धि का अवसर बना दिया। उपासक-उपासिकाएँ इस दिन “अष्टशील” ग्रहण कर संयमित दिनचर्या अपनाते हैं।
उपोसथ का उद्देश्य केवल व्रत या दिनचर्या नहीं, बल्कि अरहंत की तरह एक दिन व्यतीत करने की साधना है। इसके बारे में यह लेख पढ़ें 👉 उपोसथ क्या है?
यह धम्म के प्रति नया संकल्प, आचरण में विशुद्धि, और ध्यान में गहराई लाने का दिन है। यह दिन आत्मपरीक्षण, काय-मन-वचन की शुद्धि, दान-पुण्य, और धम्म की ऊर्जा से युक्त होता है। यही कारण है कि स्वयं बुद्ध ने गृहस्थों को यह दिवस मनाने की प्रेरणा दी, और भिक्षुओं के लिए इसे अनिवार्य कर्तव्य बनाया।
भिक्षुओं, आठ अंगों से युक्त उपोसथ को धारण करना महाफलदायी, महालाभदायी, महाज्योतिमान, महाव्यापक होता है।
— अंगुत्तरनिकाय ८:४१
भिक्षुसंघ के लिए उपोसथ का विशेष महत्त्व है। पूर्णिमा और अमावस्या को संघ एकत्र होकर पातिमोक्ख का पाठ करता है—जो कि भिक्षु-विनय के २२७ नियमों की सामूहिक स्वीकृति और आत्मावलोकन की प्रक्रिया है। यदि कोई भिक्षु अपराध करता है, तो वह इस सभा में उसे स्वीकार करता है, और संघ के प्रति आत्मशुद्धि की प्रक्रिया पूरी करता है। इसे “उपोसथ-सङ्घकम्म” कहा जाता है, और यह संघ की शुद्धता बनाए रखने का मूल आधार है।
धुतङ्ग / धुतांग
धुतांग का अर्थ हैं, ऐसा अभ्यास जो हिला-हिलाकर (क्लेष, मल) निकाल दें। ये तेरह विशिष्ट तपस्वी आचार होते हैं, जिन्हें भिक्षु स्वेच्छा से एक या अधिक धुतांग के रूप में अपनाते हैं, ताकि चित्त के मैल ( क्लेश ) और सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति आसक्ति को कम किया जा सके। इनका मूल उद्देश्य संयम, संतोष और आत्मसंयम का विकास करना है। तेरह धुतांग अभ्यास निम्नलिखित हैं:
- पंसुकूलिकाङ्ग – केवल फेंके गए कपड़ों (पंसुकूल) से ही सिला चीवर पहनना।
- तेचीवरिकाङ्ग – केवल तीन चीवर (संघाटि, उत्तरासङ्ग, अंतर्वासक) रखना।
- पिण्डपातिकाङ्ग – भोजन के लिए केवल भिक्षाटन पर निर्भर रहना, निमंत्रण न स्वीकारना।
- सपदानिकाङ्ग – भिक्षा मार्ग में आए प्रत्येक दाता से भिक्षा लेना, किसी को न छोड़ना।
- एकासनिकाङ्ग – दिन में केवल एक बार भोजन करना।
- पत्तपिण्डिकाङ्ग – भोजन पात्र में मिली भिक्षा को ही ग्रहण करना।
- खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग – भरपेट भोजन के बाद कुछ और न लेना।
- आरञ्ञिकाङ्ग – जंगल या निर्जन स्थानों में रहना।
- रुक्खमूलिकाङ्ग – किसी वृक्ष के नीचे निवास करना।
- अब्भोकासिकाङ्ग – खुले आकाश के नीचे रहना।
- सुसानिकाङ्ग – श्मशान या शव-दाह स्थलों में रहना।
- यथासन्ततिकाङ्ग – जो स्थान मिले वहीं संतोषपूर्वक रहना।
- नेसज्जिकाङ्ग – लेटकर न सोना, केवल बैठकर विश्राम करना।
धुतांग साधनाएँ विशेष रूप से उन भिक्षुओं और उपासकों के लिए लाभकारी मानी जाती हैं, जो अपने क्लेशों से विमुक्त होने और संसार से पूर्ण वैराग्य की ओर बढ़ने के इच्छुक हैं। महायान परंपरा में इन्हें अत्यंत कठिन माना गया है, लेकिन थेरवाद में आज भी कई भिक्षु इनका अभ्यास करते हैं। आयुष्मान महाकश्यप को धुतांग जीवन का आदर्श उदाहरण और अग्रणी माना जाता है।
ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि तेरह में से किसी भी धुतांग को अपनाने पर गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है—यहाँ तक कि अपने रक्त-संबंधी भिक्षु भाई से भी इसे छिपाकर रखना चाहिए। किंतु कभी-कभी कुछ भिक्षु विनय नियमों की अवहेलना कर सार्वजनिक रूप से धुतांग धारण करते हैं, जिससे उनके क्लेश समाप्त होने के बजाय बढ़ सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भिक्षुओं के लिए विनय का पालन अनिवार्य है, जबकि धुतांग साधना पूरी तरह से ऐच्छिक होती है।
आपत्ति
जब किसी भिक्षु द्वारा किसी विनय नियम का उल्लंघन होता है, तो इसे “आपत्ति” कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में, भिक्षु को दूसरे भिक्षु के सामने अपनी गलती को “आपत्तिदेसना” यानी खुले रूप से स्वीकार करना होता है। इस प्रक्रिया में भिक्षु बड़े विनम्रता के साथ, उकड़ू बैठकर और हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हैं और भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लेते हैं।
कुछ अपराधों का समाधान केवल स्वीकारोक्ति से हो जाता है, जबकि कुछ का समाधान त्याग या अस्थायी निलंबन द्वारा किया जाता है। हालांकि, कुछ (“पाराजिक”) अपराध इतने गंभीर होते हैं—जैसे यौन संबंध, मानव हत्या, चोरी और आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में झूठ बोलना—कि वे तुरंत और स्थायी निष्कासन का कारण बनते हैं।
अपराधों को इरादे (“चेतना”) के आधार पर भी बांटा जाता है। कुछ अपराध बिना किसी बुरे इरादे के या अनजाने में हो जाते हैं, जैसे कि गलत समय पर खाना खाना। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो चुका है, वह पाराजिक (निष्कासन) के अपराध नहीं कर सकता, लेकिन वह अन्य प्रकार के अपराध बिना बुरे इरादे के कर सकता है।
यह एक आपसी नैतिक और संघीय जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि कोई भिक्षु अकेले, स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार नैतिकता का पालन नहीं कर सकता। उसे संघ के नियमबद्ध और सुसंस्कृत विनय में ढलना होता है, जो भगवान ने स्वयं निर्धारित किया है। इस प्रणाली के द्वारा भिक्षु न केवल अपनी व्यक्तिगत गलतियों को सुधारते हैं, बल्कि संघ के सामूहिक कल्याण के लिए भी योगदान करते हैं।
नाग
बौद्ध परंपरा में नाग एक विशिष्ट सत्त्व है, जिसे प्राणी-योनि में जन्मा माना गया है, लेकिन जिसकी शक्तियाँ देवताओं के समान समझी जाती हैं। वे सामान्य पशु नहीं हैं। उनका स्वरूप साँप या अजगर जैसा दीर्घाकार हो सकता है, पर इच्छाधारी होने के कारण वे मानव रूप भी धारण कर सकते हैं।
उनकी प्रकृति चमत्कारी और अर्ध-दिव्य मानी जाती है, इसलिए बौद्ध ग्रंथों में उन्हें कभी देवताओं के समकक्ष, तो कभी उनके अधीन दिखाया गया है। वे कर्म के नियम से बंधे हैं, पर सामान्य पशुओं से कहीं अधिक चेतन और शक्तिशाली सत्त्व हैं।
नागों का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध सूत्रों में सम्मानपूर्वक मिलता है। बुद्ध को संबोधि प्राप्त होने के बाद जब घोर वर्षा हुई, तब नागराज मुचलिन्द ने अपने फण फैलाकर गौतम बुद्ध की रक्षा की। यह नागों की श्रद्धा और संरक्षण-भावना का प्रतीक है। इसी तरह अप्पलाल नाग की कथा है, जो बाद में बुद्ध का उपासक बनता है।
नाग प्रायः झीलों, नदियों, जलाशयों और पर्वतीय गुफाओं से जुड़े माने जाते हैं और अपने निवास-स्थानों के रक्षक होते हैं। वे क्रोधी और अहंकारी भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनमें श्रद्धा जागती है, तो वे विनीत, अनुशासित और धम्मपरायण बन जाते हैं।
बौद्ध साहित्य में “नाग” शब्द केवल एक जाति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रूपक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। पालि ग्रंथों में अरहंत या महान पुरुष के लिए भी “नाग” कहा गया है। अर्थात वह, जिसमें आंतरिक शक्ति, स्थिरता और भयहीनता हो। इसी कारण कहा जाता है कि जहाँ नाग विचरते हैं, वहाँ साधारण सर्प नहीं टिकते। यानी जहाँ अरहंत होते हैं, वहाँ अधम्म का वास नहीं रहता।
जब बौद्ध धर्म चीन पहुँचा, तो यही नाग स्थानीय संस्कृति में ड्रैगन के रूप में पहचाने गए। इस तरह नाग—या ड्रैगन—बौद्ध दृष्टि में केवल एक अद्भुत जीव नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण, परिवर्तन और नैतिक ऊँचाई का प्रतीक बन जाते हैं।
पवारणा
पवारणा—वर्षावास के समापन पर किया जाने वाला एक विशिष्ट भिक्षु-संस्कार है, जो आश्विन पूर्णिमा (अक्टूबर की पूर्णिमा) को संपन्न होता है। यह आत्मनिरीक्षण और पारस्परिक संवाद का अवसर होता है, जहाँ प्रत्येक भिक्षु , संघ के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर यह निमंत्रण देता है: “यदि आपने मेरे आचरण में कोई दोष देखा, सुना, या संदेह किया हो, तो कृपया बताएं—मैं उसे सुधारने को तैयार हूँ।”
यह परंपरा केवल विनय अनुशासन का औपचारिक रूप नहीं, बल्कि संघ की पारदर्शिता, विनम्रता और शुद्धि की संस्कृति को दर्शाती है। पवारणा के माध्यम से भिक्षु एक-दूसरे के प्रति खुलापन और दायित्व निभाते हैं—बिना द्वेष, केवल कल्याण की भावना से। यह आयोजन संघ के भीतर भरोसे, मैत्री और शील के सामूहिक अभ्यास का प्रतीक है।
पेत / प्रेत
पेत या प्रेत—वे सत्व जो मृत्यु के उपरांत असंतुष्ट वासनाओं, अतृप्त इच्छाओं या पापकर्मों के कारण पीड़ा और भूख की योनियों में जन्मते हैं। ‘पेत’ का शाब्दिक अर्थ है—“गया हुआ” या “छूट गया”, और यह शब्द बौद्ध साहित्य में ऐसे प्राणियों के लिए आता है जो इच्छा के जाल में फंसे रह जाते हैं, और शारीरिक मृत्यु के बाद भी उस मानसिक भूख से मुक्त नहीं हो पाते।
प्रेत योनि की अवस्था को दुर्गतिपूर्ण और दुःखद कहा गया है—जहाँ सत्व को भयंकर भूख-प्यास, भीषण भय, और दूसरों की दया पर निर्भर रहकर जीना पड़ता है। कुछ प्रेत बहुत छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते; कुछ विकराल रूप में प्रकट होते हैं, जैसे—जलती हुई आँतों वाला, काँटों से भरा मुँह, या निरंतर चीखता हुआ जीव। ये रूप उनके मानसिक संस्कारों और कर्मानुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।
भगवान प्रेत अवस्था के अनुभव का इस उपमा के साथ वर्णन करते हैं:
“जैसे किसी ऊबड़-खाबड़ भूमि पर एक (सूखा) वृक्ष हो, विरल पत्तियों से छितर-बितर छाया देने वाला। तब कड़ी धूप में एक आदमी आता है—गर्मी से बेहाल, थका-हारा, कांपता हुआ और प्यासा… वह पुरुष उस वृक्ष के ही नीचे बैठा या लेटा है, जहाँ उसे ज्यादातर पीड़ाओं की ही अनुभूति हो रही है।”
बुद्ध ने कहा कि प्रेत योनि में जन्म मुख्यतः लोभ, द्वेष और मिथ्याचरण के कारण होता है—विशेषकर लोभ और संग्रहवृत्ति। कुछ प्रेत पूर्व जीवन में दान न देने वाले, या अपने परिजनों को वंचित करने वाले होते हैं।
बाद के सम्मिलित किए गए बौद्ध ग्रंथ, जैसे “पेतवत्थु” में बताया गया है कि दान-पुण्य प्रेतों को समर्पित कर उन्हें राहत दी जा सकती है। भगवान ने गृहस्थों को बताया कि अपने पूर्वजों के नाम पर श्रमणों और ब्राह्मणों को अन्न आदि दान देना—प्रेत योनि में गए प्रियजनों के लिए हितकारी हो सकता है।
भव / अस्तित्व
भव का शाब्दिक अर्थ है—अस्तित्व “होना” या “बनाना”। लेकिन बौद्ध दर्शन में यह एक सूक्ष्म कर्म-प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई सत्व किसी विशेष प्रकार के अस्तित्व में प्रवेश करता है। यह धारणा जीवन के सक्रिय (अस्तित्व बनाने या बनाए रखने की जद्दोजहद) और परिणामी (फलस्वरूप अस्तित्व प्राप्त होने)—दोनों ही पहलुओं को समेटती है।
त्रिविध तृष्णा में से “भव तृष्णा”—सबसे गहरी है। यह किसी के होने, बनने, या किसी पहचान को थामने की ओर ले जाती है। यह केवल मृत्यु के बाद अगला जन्म ही तय नहीं करती, बल्कि हर क्षण चित्त जिस अवस्था को पकड़ता है, वही भव बन जाता है।
इसे एक उपमा से समझें—कल्पना करें कि किसी को पार्क जाने का विचार आता है। पहले चित्त में एक अस्पष्ट-सा विचार उभरता है—“पार्क” की एक झलक, एक धारणा। फिर यह विचार एक स्पष्ट संकल्प में बदलता है। जब व्यक्ति उस संकल्प के आधार पर कार्य करता है और वास्तव में पार्क चला जाता है, तो वही स्थान उसकी वास्तविकता बन जाता है—वही उसकी दुनिया होती है जिसे वह जीता है।
उसी तरह, जब चित्त में कोई विशेष विचार, भावना या इच्छा उपजती है, तो वह चित्त को एक विशिष्ट भव या “जन्मक्षेत्र” की ओर उन्मुख करती है। उसके आधार पर उभरे संकल्प पर कार्य करने के फलस्वरूप अस्तित्व का वह क्षेत्र वास्तविक होने लगता है। यह मानसिक प्रवृत्ति उस अस्तित्व की अवस्था या क्षेत्र के साथ एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करती है—जिससे भविष्य में उसी लोक में जन्म लेने की भूमि तैयार होती है।
तीन प्रकार के “भव” बताए गए हैं:
- काम-भव—इन्द्रिय कामसुखों के स्तर पर जीने की प्रवृत्ति, जो कामलोक के जीवनों की ओर ले जाती है। अर्थात, मानव लोक और ऊपर के छह स्वर्ग।
- रूप-भव—सूक्ष्म रूप-अवस्था में स्थिर सुख या ध्यान की अवस्था, जो ब्रह्मलोक जैसे ऊँचे लोकों की ओर ले जाती है।
- अरूप-भव—निराकार, जहाँ कोई रूप नहीं होता, केवल चित्त की अवस्थाएँ होती हैं, जैसे—असीम आकाश, असीम विज्ञान, सुना आयाम इत्यादि।
भव का सरल मूल है: “मैं यह हूँ”, या “मैं यह बनना चाहता हूँ” की धारणा। यही धारणा चित्त को बांधती है—और हर “भव” अगली “जाति” (=जन्म) बन जाती है। जब यह “भव तृष्णा” का क्षय हो जाए, तब चित्त किसी बनने की ओर नहीं जाता—और वहीं संसार रुक जाता है।
“संसार” बाहर की गति है—जन्म, मृत्यु, और पुनर्जन्म का चक्र। जबकि “भव” भीतर की गति है—चित्त की प्रवृत्ति जो उस चक्र को चलाती है।
भिक्खु / भिक्षु
भिक्षु का परंपरागत अर्थ है, जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है।
इस अर्थ को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ अन्य शब्दों पर ध्यान देना होगा।
पब्बज्जा / प्रव्रज्या
प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ है—गृहस्थ जीवन का परित्याग कर बेघर होना, अर्थात् संन्यास ग्रहण करना। जो व्यक्ति अपने परिवार, संपत्ति, आजीविका, कामभोगी जीवन, सांसारिक अभिलाषाओं तथा भव–संसरण से विमुख होकर बौद्ध धम्म के अनुसार संन्यास स्वीकार करता है, वह प्रवज्जित कहलाता है; ऐसे प्रवज्जित को श्रामणेर कहा जाता है।
बौद्ध परंपरा में प्रव्रज्या ग्रहण करने हेतु न्यूनतम आयु सात वर्ष निर्धारित की गई है। प्रवज्जित श्रामणेर के लिए त्रिशरण के साथ दस शीलों का पालन अनिवार्य होता है, तथा उसे सदैव किसी योग्य आचार्य अथवा उपाध्याय के निर्देशन में रहकर शिक्षा और अनुशासन का अभ्यास करना होता है।
भगवान बुद्ध के काल में सामान्यतः श्रामणेर की प्रव्रज्या बाल्य या किशोर अवस्था के कुमारों को दी जाती थी, क्योंकि उस आयु में भिक्षुओं के संपूर्ण विनय–नियमों का वहन करना कठिन माना जाता था। किंतु जिसकी आयु बीस वर्ष या उससे अधिक होती थी, वह उपसंपदा की विधि द्वारा सीधे भिक्षु संघ में प्रविष्ट होकर भिक्षु बनता था—यही उस समय की स्वाभाविक और मान्य परंपरा थी।
उपसंपदा
यदि कोई व्यक्ति संघ में भिक्षु बनना चाहता है, तो उसके लिए अनेक पूर्व-आवश्यकताओं का पूरा होना अनिवार्य होता है—जैसे न्यूनतम तथा अधिकतम आयु-सीमा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तथा उसका पूर्व जीवन-वृत्त (उदाहरणार्थ: हत्या, ऋण-बाध्यता, राजसेवा अथवा दासत्व आदि)।
जब ये सभी शर्तें पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, तब भिक्षुसंघ सामूहिक रूप से उसकी उपसंपदा करता है, और उसी क्षण से उसे विधिवत भिक्षु के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध ने किसी व्यक्ति को भिक्षु बनाने से पूर्व स्पष्ट और कठोर शर्तें निर्धारित की हैं। यदि इनमें से कोई भी शर्त अपूर्ण हो, तो उसे भिक्षु-उपसंपदा प्रदान नहीं की जा सकती।
उपसंपन्न भिक्षु के लिए विनय पातिमोक्ष के २२७ मूल नियमों के अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म और व्यापक विनय-नियमों का पालन भी अनिवार्य है, जिन्हें तथागत ने संघ की शुद्धता और स्थायित्व के लिए स्थापित किया। यदि कोई भिक्षु चार पाराजिका अपराधों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है, तो वह तत्काल भिक्षु-जीवन से च्युत हो जाता है और उसे जीवन-पर्यंत पुनः भिक्षु नहीं बनाया जा सकता।
अट्ठकथाओं में बुद्धघोष भंते यह उदार व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि सतिपट्ठान की साधना प्रत्येक व्यक्ति—भिक्षु या गृहस्थ—द्वारा की जा सकती है, इसलिए जब भगवान बुद्ध ने इस विशेष सूत्र को भिक्षुओं के लिए संबोधित किया, तब उसकी व्यावहारिक परिभाषा में सामान्य साधक भी सम्मिलित माने जा सकते हैं। यह व्याख्या ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद रही है—इसका विरोध भी हुआ और कालांतर में इसका दुरुपयोग भी देखा गया।
भगवान बुद्ध के समय अनेक गृहस्थ साधक अनागामी थे। उदाहरणस्वरूप, चित्त गहपति जैसे गृहस्थ, जो समाधि-स्कन्ध में परिपक्व होकर भिक्षुओं के गूढ़ प्रश्नों का समाधान किया करते थे। फिर भी, ऐसे अनागामी गृहस्थ स्वयं को न तो भिक्षु मानते थे और न ही स्वयं को भिक्षुओं से श्रेष्ठ समझते थे।
इसके विपरीत, आज के समय में कुछ गृहस्थ ध्यान-साधना के आधार पर न केवल स्वयं को भिक्षु मानने लगते हैं, बल्कि साधारण भिक्षुओं से भी श्रेष्ठ समझने का भाव पाल लेते हैं। जबकि साधना का वास्तविक उद्देश्य अहंकार का पोषण नहीं, बल्कि विपस्सना की वृद्धि है।
हिरी / ओतप्प
हिरी (=लज्जा, संकोच) एक आंतरिक भावना है, जो हमें अपने तुच्छ कर्मों के प्रति शर्मिंदा करती है। यह आत्म-सम्मान की भावना से उत्पन्न होती है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें गलत कार्यों से रोकती है।
ओतप्प (=भयभीरुता, फिक्र) अपने बुरे कर्मों के परिणामों का भय है। यह चिंता हमें भविष्य में मिलने वाली सजा और पापों के फल से डराती है, और हमें सुरक्षित एवं सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।
बुद्ध ने हिरी और ओतप्प को ‘लोकपाल’ (=संसार के रक्षक) कहा, क्योंकि ये दुनिया में नैतिकता और सदाचार बनाए रखते हैं। ये पाप को रोकने का कार्य करते हैं और मदमस्त या असंयमित व्यक्ति को गिरने से रोकते हैं। ये हमारे लिए ऐसे कर्मों के द्वार बंद कर देते हैं, जो निचले लोकों की ओर खुलते हैं।
चूँकि ये दोनों इंद्रिय हैं, इनकी शक्ति व्यक्तिगत स्तर पर भिन्न हो सकती है और इसे साधना से बलवान बनाया जा सकता है। ये शक्ति हमें सही और गलत का अंतर समझने में मदद करती है, और उद्देश्य प्राप्त करते हुए उचित और नैतिक तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
लोकधम्म
लोकधम्म आठ होते हैं—
- लाभ-हानि,
- यश-अपयश,
- निंदा-प्रशंसा,
- सुख-दुःख।
भगवान के अनुसार ये आठ लोकधम्म दुनिया के गोल-गोल घूमते हैं, और दुनिया भी इन्हीं आठ लोकधम्मों के गोल-गोल चक्कर काटती है।
ब्रह्मविहार
ब्रह्मविहार का अर्थ है—चित्त की ऐसी अवस्था या भावदृष्टि, जिसे यदि इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह सभी जीवों तक असीमित फैले, तो वह एक अत्यंत शुद्ध, शक्तिशाली और उच्च चेतना की अवस्था बनती है। यह विकसित चित्त-अवस्था किसी को ब्रह्मलोक में पुनर्जन्म के योग्य बनाती है। ३१ लोक देखें।
ये चार हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से “चार ब्रह्मविहार” कहा जाता है:
- मेत्ता—असीम सद्भावना या शुभेच्छा, जो किसी के प्रति राग या पक्षपात से मुक्त होती है।
- करुणा—असीम करुणा, जो दूसरों के दुःख को देखकर उस दुःख से मुक्ति की भावना रखती है।
- मुदिता—असीम हर्ष, अर्थात दूसरों के सुख या सफलता को देखकर ईर्ष्या रहित हर्ष का अनुभव।
- उपेक्खा—असीम तटस्थता या समभाव, जो संसार के सुख-दुःख, लाभ-हानि आदि द्वंद्वों में संतुलन बनाए रखती है, या दूसरे सत्वों के पाप-पुण्य में समभाव बनाए रखती है।
ये चारों स्वभाव केवल सामाजिक गुण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दायित्व भी हैं, जो न केवल दूसरों को सुख और राहत पहुँचाती हैं, बल्कि साधक को विमुक्ति के समीप भी ले जाती हैं।
इसकी साधना इस तरह करें 👉 🧘 मेत्ता भावना
ब्रह्मा
आम तौर पर लोग ब्रह्मा को दुनिया का रचेता, सब कुछ चलाने वाला सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। माना जाता है कि उसी की शक्ति से यह संसार बना है और वही सब जानता-देखता है। लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण इससे कुछ अलग है।
बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मा कोई ईश्वर नहीं, बल्कि ऊँचे स्तर का एक सत्व है। जैसे मनुष्य, देव, पशु आदि होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा भी एक ऊँचे श्रेणी का सत्व है जो अपने अच्छे कर्मों और गहरी ध्यान-साधना के कारण ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। वह वहाँ पहले पैदा हो जाता है, अकेला रहता है, और जब दूसरे सत्व बाद में वहाँ जन्म लेते हैं तो वे उसे सबसे पहला और सबसे बड़ा मान लेते हैं। इसी गलत समझ से उसे “सृष्टिकर्ता” समझ लिया जाता है। गहराई से जानने के लिए मज्झिमनिकाय ४९ और दीघनिकाय १ पढ़ें।
बुद्ध बताते हैं कि ब्रह्मा भी अनित्य है। उसकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन स्थायी नहीं। जब उसके पुण्य खत्म होते हैं, तो वह ब्रह्मलोक से नीचे गिरकर फिर किसी निचले लोक में जन्म ले सकता है। यानी ब्रह्मा भी जन्म-मरण और कर्म के नियम से बंधा है—न वह सर्वज्ञ है, न मुक्त, और न ही अंतिम शरण। ब्रह्मा के ज्ञान और उसकी सीमाओं को साफ़ तौर पर दीघनिकाय ११ में हास्य के साथ समझाया गया है। ब्रह्मा अवस्था पाने के लिए ब्रह्मविहार की साधना बतायी जाती है।
ब्राह्मण
ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है, जो ब्रह्मा से सुर मिलाकर, सामंजस्यता बिठाकर उसी के नियमों से चलता है।
ब्राह्मण परंपरा वेदों और शास्त्रों पर आधारित थी, जिसमें ब्राह्मण मुख्यतः यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक रीति-रिवाजों में विश्वास करते थे। वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य था, जो उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता था। धार्मिक समारोहों में उनकी प्रधान भूमिका होती थी, और उनका जीवन वैदिक सिद्धांतों और सामाजिक नियमों के अनुसार संचालित होता था।
ब्राह्मण लोगों का दावा रहता था (शायद आज भी हो) कि “ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी हीन वर्ण हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल (=उजला) वर्ण है, बाकी कृष्ण (=काला) वर्ण हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध हैं, बाकी नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा से जन्में, ब्रह्मा से निर्मित, ब्रह्मा के (असली) वारिस हैं।”
ब्राह्मणों के लिए जाति, चतुर्वर्ण व्यवस्था और परंपराओं का पालन अनिवार्य था। उससे उन्हें सामाजिक स्थिरता और धार्मिक अनुशासन को बनाए रखने में सहायता मिलती थी। हालांकि, ब्राह्मण वादी लोग अक्सर वेदों की सीमित चौखट में रहकर पक्षपाती ढंग से उनका बचाव करते थे, और उन पर प्रश्नचिन्ह उठाने वालों को अक्सर बदनाम करते थे। जिससे यह स्पष्ट होता था कि उनका दृष्टिकोण धार्मिक के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के प्रति अधिक समर्पित था।
विशेषज्ञों का कहना है कि पालि में ‘ब्राह्मण’ शब्द संस्कृतिकरण के प्रभाव से आया है। मूल शब्द वास्तव में बामन होना चाहिए, जो प्राकृत या शुरुआती लोकभाषाओं में प्रयोग होता था। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान कई स्थानों पर भाषाई परिवर्तन हुए, जिनमें न को ण में परिवर्तित करना प्रमुख है। इस परिवर्तन का उद्देश्य भाषा को अधिक शास्त्रीय और संस्कृत के निकट बनाना था, ताकि धम्म और परंपराओं का प्राचीनतम रूप से संबंध दिखाया जा सके।
वेदों ने कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन उसका महत्व सीमित और वर्णन में अर्थहीन था। वे कहते थे कि उचित कर्म मरणोपरांत अगले जीवन में सुख देते हैं, लेकिन ये उचित कर्म केवल वेद-मान्य कर्मकांड थे, जैसे यज्ञ, हवन, और बलि। केवल ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दी जाती थी और उनसे ही कर्मकांड कराए जाते थे। उनके अनुसार, कर्मकांड सही ढंग से करना अत्यावश्यक था, जिसके लिए विशेष मैनुअल और सूत्र बनाए गए थे। इस प्रकार, ब्राह्मणों के कर्म सिद्धांत का अर्थ केवल सामाजिक स्तर पर की गई शारीरिक क्रियाओं तक सीमित था।
बौद्ध धम्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने ‘ब्राह्मण’ शब्द का पुनर्परिभाषा की, जिसमें उन्होंने आंतरिक शुद्धता, नैतिकता और आत्म-ज्ञान को प्राथमिकता दी। बुद्ध ने यह बताया कि केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है; बल्कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं, जो अपने कार्यों और विचारों से शुद्धता प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण ने ब्राह्मण परंपरा को चुनौती दी और व्यक्तिगत आचार-विचार को महत्वपूर्ण माना, जिससे एक नए आध्यात्मिक विमर्श की शुरुआत हुई। बुद्ध के इस विचार ने समाज में ब्राह्मणों की पारंपरिक छवि को फिर से परिभाषित किया और आत्मिक विकास को केंद्रीय महत्व दिया।
गन्धब्ब / गन्धर्व
गंधर्व शब्द के दो प्रमुख अर्थ हैं:
- एक प्रकार के सत्व जो निचले देवलोक में वास करते हैं। ये प्रायः नृत्य-संगीत में रमे रहते हैं और कामुक प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं। उन्हें ऊँचे (तैतीस) देवताओं की सेवा में नियुक्त किया जाता है।
- एक विशेष अवस्था, जो मानवलोक में जन्म लेने से ठीक पहले की होती है।
उदाहरणस्वरूप, पञ्चशिख नामक गंधब्ब पालि साहित्य में प्रसिद्ध हैं—वे वीणा बजाते और मधुर गीत गाते हुए चित्रित किए जाते हैं। इसी तरह, धतरट्ठ (धृतराष्ट्र) को गंधब्बों का अधिपति तथा पूर्व दिशा का अधिदेवता माना गया है।
वहीं दूसरी ओर, कुछ सूत्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जब कोई ऋतुमती स्त्री पुरुष के साथ सहवास करे और उस क्षण गंधब्ब की उपस्थिति भी हो, तभी गर्भधारण संभव होता है—अन्यथा नहीं।
अर्थात, जो सत्व अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मानव जन्म के लिए तैयार हो, वह एक ऐसी विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ से वह अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर जन्म ले सकता है। इस सन्दर्भ में ‘गंधब्ब’ जन्म-जागृति की उस सूक्ष्म मध्यावस्था को भी सूचित करता है, जो जीवन के एक लोक से दूसरे लोक में जाने के बीच होती है।
देव / देवता
देव का अर्थ है—ऐसे दीप्तिमान सत्व, जो पुण्य के फलस्वरूप सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक आयु, सौन्दर्य, सुख और सामर्थ्य से युक्त होते हैं। यह कोई परम स्थिति नहीं, बल्कि एक दिव्य, परंतु अस्थायी अवस्था है—जैसे यक्ष, तावतिंस, तुषित, ब्रह्मा आदि लोक के देवता। अधिक जानकारी के लिए ३१ लोक देखें।
बुद्ध ने कहा: जो व्यक्ति श्रद्धा, शील, दान और ध्यान में कुशल होता है, वह मरणोपरांत देवयोनि को प्राप्त कर सकता है—किन्तु यह निर्वाण नहीं। देवता भी अनित्य हैं, और उनके चित्त में भोग और अशुद्धि के अंश शेष बचे रहते हैं। इसलिए बुद्ध ने देव-स्थिति को स्वीकार किया, पर उससे वैराग्य की प्रेरणा दी।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए २२ प्रतिज्ञाओं में एक है कि—“मैं हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करूँगा।” कुछ नवबौद्ध लोग इस प्रतिज्ञा को इस रूप में लेते हैं कि जैसे देवता होते ही नहीं हैं, सब अंधविश्वास है।
लेकिन यह दृष्टिकोण स्वयं बाबासाहब की मूल भावना से मेल नहीं खाता। उनकी प्रतिज्ञा हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तिपूजा और कर्मकांड पर आधारित भक्ति की अस्वीकृति थी, न कि बौद्ध परंपरा में उल्लेखित देवों के अस्तित्व को ही नकार देना।
यदि किसी नेत्रवान ने कुएँ का गंदा पानी न पीने की सलाह दी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पानी पीना ही छोड़ देना चाहिए—बल्कि शुद्ध जलस्रोत ढूँढना चाहिए। समझें कि यहाँ देवों के “अस्तित्व” का नकार नहीं, “विकृति” का है।
बौद्ध धम्म में देवता और मनुष्य दोनों त्रिरत्नों की शरण जाते हैं। इसलिए पुजा और उपासना के विषय न देव हैं, न ही मनुष्य—बल्कि धम्म का अभ्यास है, जिससे दैवत्व तो क्या, निर्वाण की राह खुलती है।
याद रखें कि देवों और स्वर्ग को नकारना न बुद्ध-वाणी है, न आंबेडकर-विचार। यह विचार मूल बौद्ध धम्म और आंबेडकर-मत दोनों के ही साथ अन्याय है।
मण्डल
मण्डल एक सूक्ष्म जगत का प्रतीकात्मक चित्र होता है, जिसका उपयोग तांत्रिक बौद्ध समुदाय में शक्तिचक्र, ध्यान और अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। मंडल जटिल ज्यामितीय संरचनाओं से बना होता है, जो ब्रह्मांड और आंतरिक चेतना के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है।
ध्यान और अनुष्ठानों में, साधक मंडल का उपयोग एकाग्रता बढ़ाने और आत्मबोध को गहराने के लिए करते हैं। इसे देखने और चिंतन करने से चित्त स्थिर होता है, आंतरिक विक्षेप कम होते हैं, और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। तांत्रिक बौद्ध परंपरा में, रेत से बने अस्थायी मंडल अनित्यता के सिद्धांत को भी दर्शाते हैं, जिन्हें अंत में विसर्जित कर दिया जाता है।
मार
मार का सरल अर्थ है, वह “जो अंततः मृत्यु का कारण बनता है” अथवा “जो अमृत धम्म (निर्वाण) से वंचित रखता है।”
प्रारंभिक सुत्तों में पाँच प्रकार के मार बताए गए हैं:
- किलेस मार – लोभ, द्वेष, मोह जैसे मानसिक क्लेश , जो व्यक्ति के चित्त को मलिन कर देते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं।
- अभिसंङ्खार मार – पुराने संस्कार का प्रभाव, जो पुनर्जन्म के चक्र में बांधता है और जन्म-मरण की निरंतरता बनाए रखता है।
- खन्ध मार – पाँच खन्ध (रूप, वेदना, नजरिया, संस्कार, और विज्ञान), जो आसक्ति पैदा करते हैं और स्थिरता का मिथ्या बोध देते हैं।
- मरण मार – मृत्यु, जो जीवन के सभी अनुभवों और अर्जित उपलब्धियों को समाप्त कर देती है, जिससे व्यक्ति फिर से पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करता है।
- देवपुत्र मार – यह देवलोक में प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट पद है। इसे थोड़ा विस्तार से समझें।
देवपुत्र मार
प्रायः यह धारणा प्रचलित है कि ‘मार’ केवल एक काल्पनिक चरित्र है या मात्र बुराई और अकुशलता का प्रतीक है। किन्तु, जब हम प्राचीन बौद्ध सूत्रों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो एक भिन्न सत्य सामने आता है। मार कोई कल्पना नहीं, बल्कि मुक्ति मार्ग में बाधा डालने वाला एक जीता-जागता अदृश्य सत्व है।
उसकी सबसे बड़ी कूटनीति यही है कि लोग उसके अस्तित्व को केवल एक वहम मानते रहें, ताकि वह परदे के पीछे छिपा रहकर सबकी डोर खींचता रहे।
‘मार’ का पद वास्तव में उस पुण्यशाली यक्ष को प्राप्त होता है, जो अतीत के पुण्यों के कारण विशेष महाऋद्धियों से संपन्न हुआ हो। इन अलौकिक शक्तियों के माध्यम से वह:
- समस्त प्राणियों के मन को पढ़ सकता है।
- लोगों की नितांत निजी दुर्बलताओं को जान लेता है।
- किसी के भी मन में विचार रोपित कर या उनके शरीर में विशेष आस्रव (दूषित ऊर्जा) प्रवाहित कर उन्हें प्रेरित, प्रभावित या पूर्णतः नियंत्रित कर सकता है।
असीमित शक्ति अक्सर चित्त को दूषित कर देती है। यही महाशक्ति मार के भीतर सत्ता की लोलुपता को जागृत करती है। फलस्वरूप, वह देव-सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी कुटिल शक्तियों को संगठित करता है और ऐश्वर्यशाली देवताओं के समानांतर अपनी स्वयं की ‘काली सत्ता’ संचालित करने लगता है।
मार का मूल उद्देश्य सभी प्राणियों को संसार-बंधन में जकड़े रखना है। उसका तर्क स्पष्ट है—यदि सभी सत्व मुक्त हो गए, तो उसका प्रभुत्व किस पर रहेगा?
इसी कारण, जब भी कोई साधक वैराग्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है, मार अनेक बाधाएँ उत्पन्न करता है। वह साधकों को भ्रमित कर उन्हें पुनः हिंसा, वासना और अज्ञान के ‘मिथ्याधम्म’ में धकेलने का प्रयास करता है।
मार का वश और उसकी माया इतनी सूक्ष्म है कि जैसा ब्रह्म निमंत्रण सूत्र में वर्णित है, स्वयं महाब्रह्मा भी उसके प्रभाव को पहचान नहीं पाते।
किन्तु, वह बुद्ध की तीक्ष्ण दृष्टि से ओझल नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध उसकी कृष्ण-प्रवृत्तियों (काले कारनामों) को भली-भांति जानते हैं, इसीलिए वे उसे ‘कान्हा’ (अर्थात् काला) और कभी-कभी उसके वास्तविक प्राचीन नाम ‘नमुची’ से संबोधित करते हैं।
यक्ख / यक्ष
बौद्ध साहित्य में यक्षों का उल्लेख विविध रूपों में होता है। वे चातुर्महाराजिक देवलोक के अधीन सत्व हैं, जो जम्बूद्वीप के उत्तर में स्थित “उत्तरकुरु” नामक अदृश्य क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसकी राजधानी आलकमंदा है। उनके अधिपति “वेस्सवण” (=वैष्णव) या कुबेर हैं, जो यक्षों के महाशक्तिशाली राजा माने जाते हैं।
कुछ यक्ष मानवों के आसपास के वनों, वृक्षों, श्मशानों या निर्जन स्थलों में भी रहते हैं। वे अदृश्य सत्व होते हैं—कभी मानवीय सुलभता से भरे, तो कभी भयावह और विक्षुब्ध। उनका स्वभाव द्वैतपूर्ण होता है: कुछ यक्ष सहायक और धम्मरक्षक होते हैं, तो कुछ हिंसक और विघ्नकारी।
उनकी स्थिति कभी-कभी “देव-योनि” और “प्रेत-योनि” के बीच की मानी गई है। वे विशेष स्थानों के रक्षक माने जाते हैं, और कुछ स्थलों पर स्थानीय देवता के रूप में पूजे भी जाते हैं—लेकिन बौद्ध धम्म में यह पूजा श्रद्धा या भय से नहीं, बल्कि सम्मान और शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के भाव से होती है।
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यक्ष एक “अदृश्य” भौतिक अवस्था भी होती है। जब कोई भी सत्व, चाहे वह देवराज इन्द्र हो, दूसरे भले देवता हो, या मार , एक विशेष अवस्था में आकर भगवान से मिलते थे, तो भगवान उन्हें “यक्ष” ही कहते हैं।
तंत्रयान बौद्ध परंपरा के “महामायूरीविद्याराज्ञी” सूत्र में यक्षों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो भारत के विभिन्न नगरों में निवास करते हैं और बुद्धधम्म की रक्षा करते हैं। उदाहरणस्वरूप, राजगृह में वकुल यक्ष, वैदिशा में वासव यक्ष, और अलकावती में वेस्सवण यक्ष का निवास बताया गया है। इन यक्षों को धम्मरक्षक और करुणासम्पन्न माना गया है।
लोकधातु
लोकधातु प्रारंभिक बौद्ध सूत्रों में उपयोग हुआ एक मूल ब्रह्माण्डीय शब्द है, जो एक पूर्ण “विश्व-प्रणाली” को दर्शाता है। इसमें एक पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा, अन्य ग्रह-पिंड, तथा काम, रूप और अरूप—तीनों स्तरों के लोक सम्मिलित माने जाते हैं। बुद्धों के प्रकट होने, उनके प्रभाव-क्षेत्र और उपदेश की सीमा को समझाने के लिए लोकधातु की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है।
सूत्रों में लोकधातु का उल्लेख एक लोकधातु, हजार लोकधातु और महासहस्सी (१००००) लोकधातु जैसे स्तरों पर मिलता है, जिससे बौद्ध दृष्टि में ब्रह्माण्ड की व्यापकता और बहुलता स्पष्ट होती है। एक ही लोकधातु में अनेक बुद्ध कालान्तर में उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु वे एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर प्रकट नहीं होते। तथापि, दूसरे लोकधातुओं में अन्य बुद्धों के अस्तित्व की संभावना मानी गई है, जो बाद के ग्रंथों में विकसित हुई है (जैसे महावस्तु १.१२२)।
चक्कवाळ / चक्रवाल
“चक्रवाल” की संकल्पना प्रारम्भिक बौद्ध सूत्रों में नहीं मिलती। इसका विकास सदियों बाद मुख्यतः अभिधम्म, अट्ठकथा और अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों में हुआ। इसमें संसार को एक ऐसे “विश्व-मंडल” के रूप में सोचा गया है, जो चारों ओर से एक प्राकृतिक सीमा में बँधा हुआ है—यानी एक तरह का बंद ब्रह्माण्ड।
इस कल्पना के अनुसार, चक्रवाल के बीचों-बीच सुमेरु पर्वत है। इसके चारों दिशाओं में चार महाद्वीप—जम्बुद्वीप, पूर्वविदेह, अपरगोडानिय और उत्तरकुरु—अपने-अपने समुद्रों और उपद्वीपों के साथ फैले हुए माने जाते हैं। सूर्य और चन्द्रमा सुमेरु के चारों ओर घूमते हुए दिन-रात और महीनों का चक्र बनाते हैं। पूरे इस संसार की बाहरी हद चक्रवाल पर्वत तय करता है, जिसके बाहर न प्रकाश पहुँचता है, न इस चक्रवाल से कोई सीधा संबंध माना जाता है।
इसी ढाँचे के भीतर ३१ लोक की कल्पना की गई है—जो नीचे के दुखप्रधान लोकों से लेकर ऊपर के सूक्ष्म और दीर्घायु देवलोकों तक फैले हैं। ये लोक किसी भौगोलिक नक़्शे की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की अलग-अलग अवस्थाओं के रूप में सोचे गए हैं।
ध्यान देने की बात यह है कि भगवान बुद्ध ने न तो इस तरह की ब्रह्माण्ड-रचना का उपदेश दिया, न ही ऐसी कल्पनाओं को मुक्ति के लिए उपयोगी माना। आधुनिक खगोल-विज्ञान के आलोक में भी स्पष्ट है कि चक्रवाल कोई वास्तविक ब्रह्माण्ड-वर्णन नहीं, बल्कि उत्तरकालीन परंपरा में विकसित एक प्रतीकात्मक और कल्पनात्मक मॉडल है।
सुमेरु / मेरु
सुमेरु पर्वत उत्तरकालीन बौद्ध ब्रह्माण्ड-कल्पना में संसार के केंद्र में स्थित एक दिव्य पर्वत माना गया है। इसे “लोक का अक्ष” कहा जाता है—एक ऐसा मध्यबिंदु, जिसके सापेक्ष ऊपर-नीचे और चारों दिशाओं में लोकों की स्थिति समझाई जाती है। चक्रवाल की पूरी रचना इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।
परंपरागत वर्णनों में सुमेरु को स्वर्ण, रजत और रत्न जैसी दिव्य धातुओं से बना बताया गया है। इसकी चोटी पर तैंतीस (“तावतिंस”) लोक है, जहाँ देवराज इन्द्र (सक्क) का निवास माना जाता है। इसके नीचे कामधातु के लोक आते हैं—जिनमें मनुष्य-लोक, पशु-लोक, प्रेत-लोक और नरक शामिल हैं। सुमेरु से ऊपर क्रमशः रूपधातु और अरूपधातु के सूक्ष्म देवलोक बताए गए हैं। इस तरह, इकतीस लोक नीचे से ऊपर तक एक क्रम में समझे जाते हैं।
लेकिन सुमेरु को केवल एक काल्पनिक पर्वत मान लेना बात को अधूरा छोड़ देता है। यह संसार की नैतिक और मानसिक संरचना का भी प्रतीक है—जहाँ ऊपर की दिशा शुद्ध चित्त, कुशल कर्म और शांति की ओर संकेत करती है, और नीचे की दिशा तृष्णा, अज्ञान और दुख की ओर। इस दृष्टि से सुमेरु वह प्रतीकात्मक केंद्र है, जिसके सापेक्ष संसार चलता रहता है—और जहाँ ऊपर उठने का मार्ग धम्म है, जबकि गिरने का कारण तृष्णा और अविद्या।
३१ लोक
बौद्ध परंपरा में अस्तित्व को ३१ लोकों में बाँटकर समझाया गया है। ये लोक किसी नक़्शे पर बनी जगहें नहीं हैं, बल्कि चेतना और कर्म के अनुसार अनुभव की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। मोटे तौर पर इन्हें तीन स्तरों में समझा जाता है: कामधातु, रूपधातु और अरूपधातु।
| धातु | क्रम | स्तर | लोक | संक्षिप्त टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| काम-धातु | १ | अपाय | नरक | घोर यातना |
| 〃 | २ | अपाय | पशु | अज्ञान, भय और अस्तित्व के लिए संघर्ष |
| 〃 | ३ | अपाय | प्रेत | अतृप्त रहते हुए भटकना |
| 〃 | ४ | अपाय | असुर | अहंकार, ईर्ष्या, संघर्ष, शैतानी वृत्ति, षड्यंत्रकारी मन। |
| 〃 | ५ | मनुष्य | मनुस्स-लोक | सुख-दुःख का बेजोड़ संतुलन; धर्माभ्यास की सर्वोत्तम संभावना। |
| 〃 | ६ | देव | चातु-महा-राजिक | गन्धब्ब, कुंभण्ड, नाग, यक्ष पूर्व-दिशा में गन्धर्वों का महाराज धृतराष्ठ दक्षिण दिशा में कुंभण्डों का महाराज विरुल्हक पश्चिम दिशा में नागों का महाराज विरूपाक्ष और उत्तर दिशा में यक्षों का महाराज कुबेर या वैष्णव! |
| 〃 | ७ | देव | तावतिंस | देवराज इन्द्र और ३३ देवता। |
| 〃 | ८ | देव | याम | स्थूल सुख से मुक्त |
| 〃 | ९ | देव | तुसित | संतुष्ट सत्व |
| 〃 | १० | देव | निम्मान-रति | स्वयं से रचित निर्माणों पर खुश रहने वाले। |
| 〃 | ११ | देव | पर-निम्मित-वसवत्ति | दूसरों के रचे निर्मिति पर वश करने वाले। |
| रूप-धातु | १२ | प्रथम-ध्यान | ब्रह्म-पारिसज्ज | ब्रह्मा का समुदाय |
| 〃 | १३ | प्रथम-ध्यान | ब्रह्म-पुरोहित | ब्रह्मा के सहचर |
| 〃 | १४ | प्रथम-ध्यान | महा ब्रह्मा | दीर्घायु, सूक्ष्म अहं। यहाँ से आगे ब्रह्मा किसी एक लोकधातु में सीमित नहीं रहता, बल्कि हजारो-लाखों लोकधातुओं में व्याप्त होता है। |
| 〃 | १५ | द्वितीय-ध्यान | परित्ताभा | सीमित प्रकाश |
| 〃 | १६ | द्वितीय-ध्यान | अप्पमाण-आभा | असीम प्रकाश |
| 〃 | १७ | द्वितीय-ध्यान | आभस्सर | उज्ज्वल चेतना |
| 〃 | १८ | तृतीय-ध्यान | परित्त-सुभा | सीमित शुद्धता |
| 〃 | १९ | तृतीय-ध्यान | अप्पमाण-सुभा | असीम शुद्धता |
| 〃 | २० | तृतीय-ध्यान | सुभकिण्ह | शांत, स्थिर अवस्था |
| 〃 | २१ | चतुर्थ-ध्यान | वेहप्पल | महान कर्मफल |
| 〃 | २२ | चतुर्थ-ध्यान | असञ्ञ-सत्त | संज्ञारहित जन्म। कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। |
| 〃 | २३ | चतुर्थ-ध्यान | अविहा | शुद्धावास। यहाँ और यहाँ से आगे अकनिट्ठ तक केवल अनागामी ही पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद फिर कभी दुबारा जन्म नहीं होता। |
| 〃 | २४ | चतुर्थ-ध्यान | अतप्पा | शुद्धावास |
| 〃 | २५ | चतुर्थ-ध्यान | सुदस्सा | शुद्धावास |
| 〃 | २६ | चतुर्थ-ध्यान | सुदस्सी | शुद्धावास |
| 〃 | २७ | चतुर्थ-ध्यान | अकनिट्ठ | सर्वोच्च शुद्धावास |
| अरूप-धातु | २८ | अरूप | आकाशा-नञ्चायतन | आकाश की अनंतता। यहाँ न कोई भौतिक रूप होता है, न ही इंद्रिय। |
| 〃 | २९ | अरूप | विञ्ञाण-ञ्चायतन | चेतना की अनंतता |
| 〃 | ३० | अरूप | आकिञ्च-ञ्ञायतन | शून्यता का अनुभव |
| 〃 | ३१ | अरूप | नेवसञ्ञा-नासञ्ञा-यतन | अत्यन्त सूक्ष्म चित्त |
इन लोकों को ऊपर–नीचे बनी मंज़िलें न समझकर, कर्म और चित्त की अवस्था के रूप में समझना ज़्यादा सही है।
- अकुशल कर्म → नीचे के लोक
- कुशल कर्म → ऊँचे लोक
- लेकिन मुक्ति (निब्बान) → इन ३१ लोकों से भी परे
इसीलिए बुद्ध का लक्ष्य किसी ऊँचे लोक में जन्म लेना नहीं, बल्कि पूरे इस चक्र से मुक्त होना है।